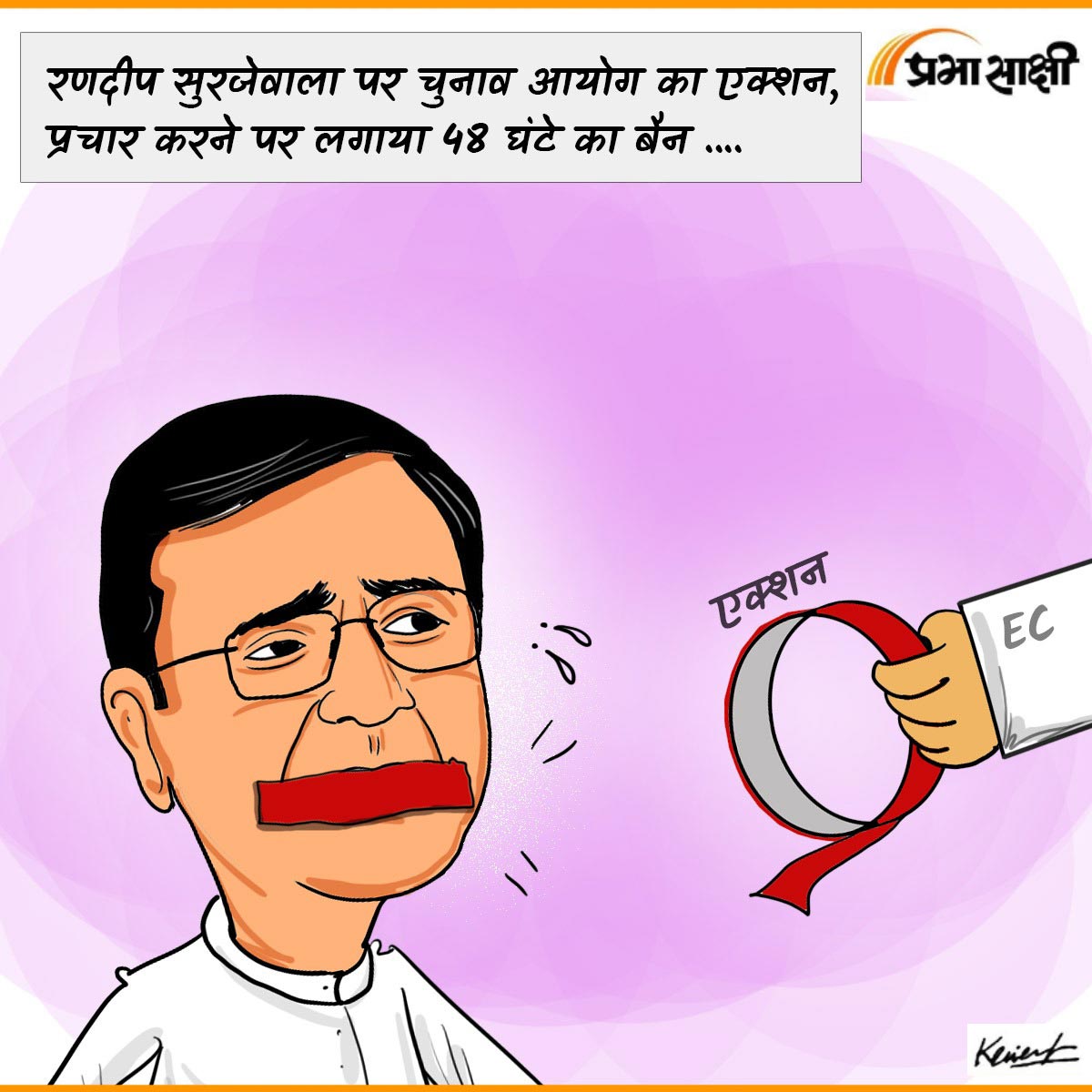आज के डिजिटल युग में छिनता जा रहा है श्रमिकों का रोजगार
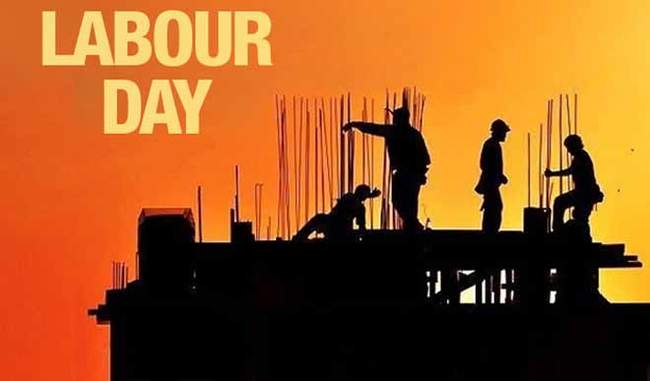
अगर कुछ बड़े मेट्रो शहरों की बात न करके छोटे कस्बों एवं गांव−देहातों की बात करें तो वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे मजदूर एवं किसान महज सौ−डेढ़ सौ रुपये ही प्रतिदिन कमा पाते हैं, वह भी दस घंटों की हाड़तोड़ मेहनत मशक्कत के बाद।
ई−प्रथा और डिजीटल युग ने श्रमिकों की जरूरत को खत्म कर दिया है। श्रमिकों के हिस्से थोड़ा−बहुत काम आता भी है तो उसका उन्हें पूरा श्रम नहीं मिल पाता। जिस प्रकार स्टीम इंजन ने लोगों का रोजगार छीन लिया, उसी प्रकार फोटो कॉपी मशीन ने टाइपिस्टों का, उबर−ओला ने टैक्सी स्टैंडों का, कम्प्यूटर ने सांख्यिकी गणित करने का और ई−मेल ने डाकिए का रोजगार हड़प लिया है। वहीं ट्यूबवेल और ट्रैक्टर ने खेत मजदूरों के नए रोजगार बनाए थे, उसी प्रकार फोटोकॉपी, कॉल सेंटर, मोबाइल डाउनलोड आदि में नए रोजगारों का सृजन हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार खेत−मजदूर की आय जुलाहे की आय की तरह न्यून बनी रही, उसी प्रकार मोबाइल हाथ में लिए हुए श्रमिक की आय न्यून बनी हुई है। इसलिए ज्यादा मेहनताना मांगना खुद में बेईमानी सा लगता है। इसलिए हिंदुस्तान की तरक्की सिक्के के दो पहलू की तरह हो गई। खुशहाल और बदहाल। दोनों की ताजा तस्वीरें हमारे समक्ष हैं। एक वह जो ऊपरी और काफी चमकीली है। इस लिहाज से देखें तो पहले के मुकाबले देश की शक्ल−व−सूरत काफी बदल चुकी है। अर्थव्यवस्था अपने पूरे शबाब पर है और कहने को तो उच्च मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग सभी खुशहाल हैं लेकिन तरक्की की दूसरी तस्वीर भारतीय श्रमिकों और किसानों की है। जिनकी बदहाली कहानी हमारे सामने है। जीतोड़ मेहनत करने के बावजूद श्रमिकों को गुजर−बसर करने लायक पारिश्रमिक तक नहीं मिल पाता।
श्रम दिवस के मौके पर श्रमिकों के लिए कई सरकारी आयोजन किए जाते हैं। इनकी बदहाली को दूर करने के लिए नेता−नौकरशाह सभी लंबे−लंबे भाषण देते हैं साथ ही तमाम कागजी योजनाओं का श्रीगणेश भी करते हैं, लेकिन महीने की दूसरी तारीख यानी दो मई के बाद में सब भुला दिए जाते हैं। हुकूमतें जानती हैं कि मजदूर अपने अधिकारों से देश आजाद होने के बाद से ही वंचित है। देखिए, कामगार तबका दशकों से पूरी तरह से हाशिए पर है। अगर कुछ बड़े मेट्रो शहरों की बात न करके छोटे कस्बों एवं गांव−देहातों की बात करें तो वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे मजदूर एवं किसान महज सौ−डेढ़ सौ रुपये ही प्रतिदिन कमा पाते हैं, वह भी दस घंटों की हाड़तोड़ मेहनत मशक्कत के बाद। उस पर तुर्रा यह कि इस बात कि कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है कि उन्हें रोज ही काम मिल जाए। इतने पैसे में वह अपने परिवार के लिए दो जून की रोटी भी बामुश्किल से ही जुटा पाता है। भारत की यह तस्वीर यहां के बाशिंदे तो देख रहे हैं लेकिन विदेशों में सिर्फ हमारी चमकीली अर्थव्यवस्था का ही डंका है। मजदूरों की हालत बहुत ही दयनीय है, सियासी लोगों के लिए वह सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय काम आने वाला एक मतदाता है। पांच साल बाद उनका अंगूठा या ईवीएम मशीन पर बटन दबाने का काम आने वाला वस्तू मात्र है।
पिछली कांग्रेस सरकार ने श्रमिकों के लिए एक योजना बनाई थी जिसमें मजदूरों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का मसौदा तैयार किया था मसलन, दैनिक मजदूरी, स्वास्थ्य, बीमा, बेघरों को घर देना। यह बात फरवरी सन् 2010 की है। लेकिन योजना हर बार की तरह कागजी साबित हुई। सबसे बड़ी बात यह कि श्रमिकों के हितों के लिए ईमानदारी से लड़ने वाला कोई नहीं है। पूर्व में जिन लोगों ने मजदूरों के नाम पर प्रतिनिधित्व करने का दम भरा जब उनका उल्लू सीधा हो गया वह भी सियासत का हिस्सा हो गए। उन्होंने भी मजदूरों के सपनों को बीच राह में भटकने के लिए छोड़ दिया। लेकिन केंद्र की मौजूदा मोदी सरकार श्रमिकों के लिए संजीदा से काम करती दिख रही है। मजदूरों के उद्धार के लिए बनाए गए लक्ष्य को हासिल करने में किसी तरह की कोताही नहीं होने देंगे की बात कही जा रही है।
श्रमिकों की बदहाली से भारत ही आहत नहीं है बल्कि दूसरे मुल्क भी पेरशान हैं। भूख से होने वाली मौतों की समस्या पूरे संसार के लिए बदनामी जैसी है। झारखंड़ में एक बच्ची बिना भोजन के दम तोड़ देती है। सवाल उठता है जब जनमानस को हम भर पेट खाना तक मुहैया नहीं करा सकते तो किस बात की हम तरक्की कर रहे हैं। भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में यह समस्या काफी विकराल रूप में देखी जा रही है। आकंड़ों के मुताबिक सिर्फ हिंदुस्तान में रोज 38 करोड़ लोग भूखे पेट सोते हैं। भारत के उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में तो भूख के मारे किसान एवं मजदूर दम तोड़ रहे हैं। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। तमाम तरह के प्रयासों के बावजूद आजतक इस दिशा में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ सका है। इसके अलावा बिहार, झारखण्ड, तमिलनाडु एवं अन्य छोटे प्रांतों के कुछ छोटे−बड़े क्षेत्र इस समस्या से प्रभावित होते रहे हैं। यह वह इलाका है जहां समाज के पिछड़ेपन के शिकार लोगों का भूख से मौत का मुख्य कारण गरीबी है। इसके विपरीत देश के कई प्रांतों में लोग भूख के बजाए कर्ज और उसकी अदायगी के भय से आत्महत्या कर रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि गरीबी के कारण भूख से मरने वाले आमतौर पर गरीब किसान और आदिवासी हैं।
श्रमिकों की दशा सुधरे इसके लिए हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है मगर इसका कुप्रंधन ही समस्या का बुनियादी कारण है। इसी कुप्रंधन का नतीजा है कि ग्रामीण श्रमिक लगातार शहरों की ओर भागने को विवश हो रहे हैं। गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रही आबादी पर अगर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि इनमें गरीब नौजवानों से लेकर सम्पन्न किसान और पढ़े−लिखे प्रोफेशनल्स तक शामिल हैं। यह तथ्य यह बताने के लिए काफी है कि जनसंख्या के इस तरह के बड़े पैमाने पर हस्तानांतरण का कारण केवल गरीबी और बेरोजगारी ही नहीं बल्कि विकास का असंतुलन है। कतार में खड़े अंतिम आदमी की बात तो हर नेता करता है लेकिन उसकी बात केवल भाषण तक ही सीमित रह जाती है। उस अंतिम आदमी तक संसाधन पहुंचाने के दावे तो खूब किए जाते हैं लेकिन पहुंचाने तक की ताकत किसी में नहीं है। शायद यही कारण है कि गांवों में स्कूल तो हैं लेकिन तालीम नदारद है, अस्पताल तो हैं लेकिन डॉक्टर व दवाईयां नहीं हैं। दूरवर्ती गांवों तक पहुंचने को सड़कें हैं लेकिन वाहन नहीं। प्रशासन है लेकिन अराजक तत्वों का उस पर इतना दबदबा है कि प्रशासन उनके आगे लुंजपुंज हो जाता है। ग्रामीण विकास का यह परिदृश्य समस्या की जटिलता को स्पष्ट करने के लिए काफी है। श्रमिकों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले इसके लिए इच्छाशक्ति की जरूरत है। श्रमिकों के हित में नई योजना नीति बनाने की दरकार है। हालांकि देखा जाए तो पिछले दो सालों से श्रमिकों के न्यूनतम दिहाड़ी को लेकर कुछ राज्य सरकारों ने वेतन सीमा निर्धारित की है। लेकिन ठेकेदार उनकी मुहिम पर पानी फेर रहे हैं।
-रमेश ठाकुर
अन्य न्यूज़