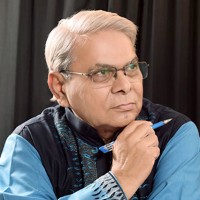जामुन की पैदावार के लिए खतरा बन सकता है छिद्रक कीट

जामुन को नुकसान पहुंचाने वाला यह एक हाइमेनोप्टेरान कीट है। यूलोफिडे परिवार के इस फाइटोफैगस (वनस्पतियों को खाने वाले) कीट का लार्वा जामुन के बीजों को खाता है। कीट से ग्रस्त बीजों की अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है, जो जामुन उत्पादकों के लिए चुनौती बनकर उभर सकता है।
नई दिल्ली।(इंडिया साइंस वायर): कीटों का आक्रमण हो जाए तो फलों की पैदावार प्रभावित होने के साथ-साथ उनका स्वाद और रंग-रूप भी बिगड़ जाता है। भारतीय शोधकर्ताओं ने जामुन के फलों के विकास के ऐसे महत्वपूर्ण चरणों का पता लगाया है, जो अनसेल्मेला केरची नामक छिद्रक कीट के प्रकोप के प्रति संवेदनशील होते हैं। इस नए शोध से मिली जानकारी इस कीट से निपटने के लिए प्रभावी रणनीति बनाने में मददगार हो सकती है।
अनसेल्मेला केरची कीट जामुन के फलों को बदरंग और बेस्वाद बनाकर नष्ट कर देता है। इन कीटों के प्रकोप से जामुन के फलों पर गहरे काले रंग के छेद हो जाते हैं और फल का 62 प्रतिशत तक हिस्सा नष्ट हो जाता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अनसेल्मेला केरची के प्रकोप से बेंगलुरु के ग्रामीण इलाकों में जामुन की फसल को बड़े पैमाने पर नुकसान होने का भी पता लगाया है।
इसे भी पढ़ें: शहरी क्षेत्रों में बाढ़ पूर्वानुमान के लिए नई प्रणाली विकसित
जामुन को नुकसान पहुंचाने वाला यह एक हाइमेनोप्टेरान कीट है। यूलोफिडे परिवार के इस फाइटोफैगस (वनस्पतियों को खाने वाले) कीट का लार्वा जामुन के बीजों को खाता है। कीट से ग्रस्त बीजों की अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है, जो जामुन उत्पादकों के लिए चुनौती बनकर उभर सकता है। बेंगलुरु के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह अध्ययन शोध पत्रिका करंट साइंस में प्रकाशित किया गया है।
अध्ययन के दौरान कीट से ग्रस्त जामुन के पेड़ों से फल एकत्रित करके उन्हें आकार, रंग, कठोरता के आधार पर पांच वर्गों में बांटा गया और फिर फलों का व्यास एवं लंबाई, बीजकोष की मोटाई और बीजों का व्यास दर्ज किया गया। करीब 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर प्लास्टिक के डिब्बों में फलों को व्यस्क कीटों के बाहर निकलने तक रखा गया। इस बीच कीटों के बाहर निकलने, फलों पर निकास छेदों की संख्या और उनका व्यास दर्ज किया गया। इसके बाद, कीटों से ग्रस्त फलों पर चीरा लगाकर उनके वास्तविक स्वरूप में हुई क्षति का आकलन किया गया है।
इसे भी पढ़ें: कम उम्र में बढ़ रहा है उच्च रक्तचाप का खतरा
फलों को चीरकर देखने पर उनमें पूर्ण रूप से विकसित 10-15 व्यस्क कीट देखे गए हैं। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि कीटों का प्रकोप फलों के चौथे और पांचवें चरण में सबसे अधिक होता है और नर कीटों की तुलना में मादा कीटों की संख्या अधिक देखी गई है। फल के बाहरी हिस्से पर उभरने वाले निकास छिद्र फल की मध्य परत से होते हुए बीज के भीतर कीट लार्वा को पोषित करने वाले केंद्र जुड़े होते हैं।
फलों के विकास के विभिन्न चरणों का साकारत्मक संबंध इन काले छिद्रों के उभरने से पाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार, फलों के विकास का दूसरा चरण इन कीटों के प्रकोप के लिए अधिक संवेदनशील होता है। इस दौरान वनस्पतियों से बने कीटनाशकों का उपयोग कीटों के प्रकोप को कम करने में मदद मिल सकती है।
जामुन सियाजियम प्रजाति का फल है। क्वींसलैंड, मलेशिया और पपुआ न्यू गिनी जैसे देशों में अनसेल्मेला वंश की दूसरी कीट प्रजातियां अनसेल्मेला मिल्टोनी, अनसेल्मेला मैलेसिया और अनसेल्मेला ओकल्ट सियाजियम प्रजाति के फलों- ब्रश चेरी, लिलि पिली और जावा ऐपल के लिए प्रमुख खतरे के रूप में देखी गई हैं।
इसे भी पढ़ें: नई तकनीकों से हल हो सकती है पराली की समस्या
बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो के डाटाबेस में जामुन को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की करीब 78 प्रजातियों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, डाटाबेस में मौजूद कीटों में से किसी का संबंध अनसेल्मेला केरची से नहीं मिलता है। इसी से पता चलता है कि इस कीट से जामुन पर पड़ने वाले दुष्परिणामों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि समय रहते इस कीट की रोकथाम न की गई तो यह जामुन की पैदावार को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है।
भारत में अनसेल्मेला केरची प्रजाति के कीट पहली बार वर्ष 1957 में पुणे में पाए गए थे। हालांकि, अनसेल्मेला केरची छिद्रक कीट के कारण जामुन को होने वाले नुकसान और इसके आर्थिक महत्व के बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया। शोधकर्ताओं में पी.डी. कमला जयंती, अंजना सुब्रमण्यम, ए. रेखा और बी. आरा. जयंती माला शामिल थे।
(इंडिया साइंस वायर)
अन्य न्यूज़