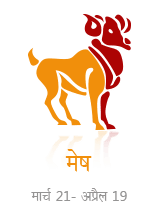Gyan Ganga: श्रीराम से सुग्रीव की भेंट कराते समय हनुमानजी के मन में आ रहे थे यह विचार

श्री हनुमान जी कितने उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक हैं। जानते हैं कि सुग्रीव तो श्रीराम जी को देख पहले ही दूर भागने का मन बना बैठे हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि मैं इशारा तो करूं कि आप यहाँ आ जाईए भयभीत होने की आवश्यक्ता नहीं और सुग्रीव कहीं उल्टा दौड़ ही न जाए।
विगत अंकों में हमने देखा कि श्री हनुमान जी प्रभु श्रीराम जी के आगे सुग्रीव का पक्ष बड़े दृढ़ भाव से रखते आ रहे हैं। आखिर सुग्रीव की ऐसी क्या विशेषता है। वास्तव में तात्विक दृष्टि का तो यही निष्कर्ष है कि सुग्रीव नींव की भूमिका में है और श्री हनुमान जी संत की भूमिका में है। जीव की दृष्टि आवश्यक नहीं कि भगवान के प्रति सदा श्रद्धा से ही सराबोर हो। जैसे सुग्रीव ने जब श्री राम जी को दूर से आते देखा तो उन्हें भगवान न जानकर उलटा उन्हें बालि द्वारा भेजे गए शत्रु ही समझ लिया। यद्यपि सुग्रीव का यह मनोभाव निःसंदेह निंदनीय है लेकिन उसका सराहनीय पक्ष यह भी है कि सुग्रीव अपने इस मनोभाव पर अडिग अथवा दृढ़ नहीं रहा। अपितु उसने समाधन तक पहुँचना चाहा। समाधन यह कि अगर मेरी दृष्टि उन दोनों वीरों को पहचानने में धेखा खा रही है तो मुझे अवश्य ही हनुमंत लाल जी की दृष्टि का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि हनुमान एक संत हैं और संत की दृष्टि ही एक ऐसी दृष्टि है जो वास्तविकता से परिचित करवा सकती है। सुग्रीव श्री हनुमान जी से यही कहते हैं कि−'हरि बटु रुप देखु तैं जाई' अर्थात ब्राह्मण रुप धरण कर आप वहाँ जाईए। सुग्रीव के इस पक्ष को हमने सराहनीय इसलिए कहा कि सुग्रीव ईश्वर के प्रति जब किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता और स्वयं को उलझा हुआ पाता है। तो अपने सारे हथियार फेंक कर बस साधु के आगे समपर्ण कर देता है। कि हे महाराज! अब बस आप ही देखिए। और मुझे तो आप केवल इशारा भर कर दीजिएगा। मैं आपके इशारे को आधर मान कर ही आगे का कदम उठाऊंगा।
इसे भी पढ़ें: Gyan Ganga: प्रभु को कंधे पर बैठाने से पहले श्रीराम और हनुमानजी का सुंदर वार्तालाप
सज्जनों जीव के साथ यही घटनाक्रम तो उसके जीवन की सफलता व विफलता को निर्धारित करता है। अपनी प्रत्येक क्रिया से पहले अगर हम परम साधु को यह अधिकार दे दें कि आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। आप ही के आदेश पर हमारे कदम उठेंगे और आप ही की आज्ञा पाकर रूकेंगे तो सच मानिएगा हमें जीवन में स्वयं का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सुग्रीव ने यही किया। वरना सुग्रीव भले ही अतिअंत बलवान व भक्त हृदय क्यों न हों
लेकिन एक निर्बल भाव उसमें सदा ही विद्यमान रहा। वह यह कि वह बड़ी शीघ्र डर जाता है। श्री हनुमान जी को भी यही कहा कि अगर वह दोनों वीर मलिन बालि के भेजे होंगे तो मैं तुरंत भाग जाऊंगा 'भागौं तुरत तजे यह सैला' फिर बालि जब मायावी राक्षस से युद्ध करते हुए एक महीने तक गुफा से बाहर नहीं आया और तब रक्त की बड़ी भारी धरा बहती हुई गुफा से बाहर निकली, तो तब भी सुग्रीव डर डर गया कि अवश्य ही मायावी ने बालि का वध कर दिया है। और अब निश्चित ही वह मुझे मारेगा। और तुरंत एक बड़ी सिला गुफा के द्वार पर लगा कर सुग्रीव वहाँ से भाग गया−
मास दिवस तहँ रहेउँ खरारी। निसरी रूधि धर तहँ भारी।।
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई। सिला देइ तहँ चलेउँ पराई।।
श्री हनुमान जी कितने उच्च कोटि के मनोवैज्ञानिक हैं। जानते हैं कि सुग्रीव तो श्रीराम जी को देख पहले ही दूर भागने का मन बना बैठे हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि मैं इशारा तो करूं कि आप यहाँ आ जाईए भयभीत होने की आवश्यक्ता नहीं और सुग्रीव कहीं उल्टा दौड़ ही न जाए। बिलकुल वैसे ही जैसे एक बालक घुटनों के भार चलता हुआ बिलकुल कुएं के किनारे पहुँच जाता है। और ऐसे में अगर उसकी माँ जोर से चिलाकर उसे डांटे तो वह डर कर दूर भागता है और कुएं में गिरता ही है। उसकी माँ उसे न भी डांटे और कहे कि आ जा, मेरा राजा बेटा मेरे पास आ जा। तब भी बालक लाड़−लाड़ में अकसरां अपनी माँ से दूर ही भागता है। और इस स्थिति में भी उसका गिरना तय ही है। लेकिन जब माँ चुपचाप बिना हड़बड़ाहट व शोर किए। उसकी तरफ जाती है तो बालक को लगता है कि माँ के लिए मैं लक्ष्य नहीं हूँ तो वह वहीं अपनी यथास्थिति में बना रहता है। और माँ धीरे से उसके पास जाकर उसे तपाक से अपने हाथों में ले लेती है। ठीक वैसे ही श्री हनुमान जी ने सुग्रीव को कोई इशारा ही नहीं किया। और सीधे बस प्रभु को पीठ पर चढाकर सुग्रीव की तरफ ले चले। क्योंकि श्री हनुमान जी जानते थे कि सुग्रीव को उन पर विश्वास है और दूर से ही जब देखेंगे कि मैंने प्रभु को अपनी पीठ पर बिठाया हुआ है। तो अपने आप ही इशारा हो जाएगा कि पीठ पर सवार दोनों वीर कोई शत्रु नहीं अपितु मित्र हैं।
साधु के वचनों अथवा क्रियाओं पर जिस जीव को ऐसे विश्वास हो फिर उसे भगवान को मिलने की अथवा ढूंढने की माथापच्ची थोड़ी करनी पड़ती है। अपितु भगवान स्वयं ही चलकर उस तक पहुँच जाते हैं। बस आप को अपने स्थान पर मात्रा बैठना ही होता है। उसके पश्चात तो सारी करामात संत की ही होती है। समीकरण ऐसे बनते हैं कि जहाँ भगवान बैठा करते हैं वहाँ भक्त बैठते हैं और भक्त के स्थान पर प्रभु को बैठना पड़ता है।
इसे भी पढ़ें: Gyan Ganga: हनुमानजी में दो हृदयों को आपस में जोड़ने की गज़ब की कला है
आप देखिए न प्रायः हमारे देवी देवताओं के मंदिर पहाड़ी के शिखर पर ही तो होते हैं। जैसे माँ वैष्णो देवी, नयना देवी या अन्य देव। जिसमें श्रद्धालु तल से ऊपर पहाड़ी की तरफ भक्ति गीत गाते चढ़ते हैं। यही हमने सब ओर सब समय और सब धर्म स्थलों पर देखा है। लेकिन सुग्रीव ने श्री हनुमान जी रूपी साधु को अपनी जीवन डोरी क्या सौंपी सारी रीतियां व नीतियां ही बदल गईं। क्योंकि प्रभु को बिराजना चाहिए पर्वत शिखर पर और बिराज रखें हैं हमारे सुग्रीव जी। फिर श्रद्धालु जैसे देव स्थल की चढाई भिन्न−भिन्न साधनों द्वारा पूरी करते हैं। ठीक वैसे ही श्रीराम जी भी श्री हनुमान जी की पीठ पर सवार हो अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं। लेकिन अपने किसी अराध्य देव की और नहीं अपितु अपने नए नवेले भक्त सुग्रीव की तरफ। देखो न साधु मिले और कैसे भक्त और भगवान के बीच भक्ति संपूर्ण के सिद्धांत ही बदल गए। आगे चलकर एक और नई रीति का प्राकटय होना है। जिसे जानेगे हम अगले अंक में...क्रमशः...
- सुखी भारती
अन्य न्यूज़