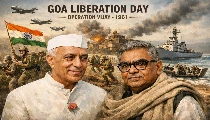ईमानदारी का बोझ (व्यंग्य)

अब बात करते हैं हमारे कहानी के नायकों की, किरण और आलोक, जो बेचारे इस 'न्याय' के मकड़जाल में फँस गए थे। उनके पिताजी, बाबू धर्मनिष्ठ, एक सच्चे और सीधे-सादे आदमी थे, जो भूल से सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहे थे।
पुराने दिनों की बात है, जब हमारे शहर में ईमानदारी एक दुर्लभ प्रजाति हुआ करती थी, जैसे आज अच्छे नेता। उस समय, एक सज्जन थे, बाबू सुखराम, जो अपने नाम के अनुरूप केवल सुख से राम नाम जपने के लायक थे, खासकर जब बात उनके आलस्य और अक्षमता की आती थी। बाबूजी एक सरकारी दफ्तर में 'अत्यंत महत्वपूर्ण' पद पर थे, जिसका अर्थ था कि वे दफ्तर में सबसे कम काम करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन सबसे ज्यादा चाय पीने वाले। उनका दिन सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त पर समाप्त होता था, और इस पूरे अंतराल में उनका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी काम बिना रिश्वत के न हो। उनकी रिश्वत भी कोई साधारण रिश्वत नहीं थी, वह तो कला का एक अनुपम उदाहरण थी। कभी दस का नोट बड़े ही नाटकीय ढंग से मेज से फिसलकर उनकी जेब में चला जाता, तो कभी बीस का नोट फाइलों के ढेर में ऐसे छिप जाता, मानो वह भी भ्रष्टाचार के अंधेरे में अपनी पहचान छिपा रहा हो। बाबूजी अक्सर कहते थे, "ईमानदारी तो बुढ़ापे की निशानी है, जवान आदमी को तो थोड़ा टेढ़ा चलना ही पड़ता है।" और वे इस सिद्धांत का पालन बड़ी निष्ठा से करते थे। उनका घर एक छोटा सा महल था, जिसकी नींव रिश्वत के ईंटों से रखी गई थी और छत भ्रष्टाचार के कंक्रीट से बनी थी। उनकी पत्नी, श्रीमती दौलत देवी, उनकी हर 'उपलब्धि' पर गर्व करती थीं। वे अक्सर मोहल्ले की औरतों से कहती थीं, "मेरे पति देव ने कभी किसी का काम बिना पैसे के नहीं किया, आखिर ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है!" और यह कहते हुए उनका सीना गर्व से फूल जाता, मानो उन्होंने कोई महान त्याग किया हो। उनके बच्चे भी इसी माहौल में पले-बढ़े, जहाँ रिश्वत एक पारिवारिक संस्कार था और बेईमानी एक पुण्य। उनके बेटे, लखपती लाल, और बेटी, करोड़पति कुमारी, को बचपन से ही सिखाया गया था कि जीवन में सफलता का एक ही मंत्र है - 'लेना सीखो, देना नहीं।' और वे इस मंत्र का पालन बड़ी ईमानदारी से करते थे, खासकर जब बात दूसरों का पैसा हड़पने की आती थी। सच कहूँ तो, उस समय हमारा समाज इतना 'पारदर्शी' था कि भ्रष्टाचार को छिपाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वह तो खुलेआम नाचता था, जैसे आज के नेता मंचों पर। उस समय, अगर कोई ईमानदार अधिकारी गलती से आ भी जाता, तो उसे ऐसे देखा जाता, जैसे वह किसी और ग्रह से आया हो, या शायद उसका दिमागी संतुलन ठीक न हो। लोग कहते थे, "अरे, यह ईमानदार है? लगता है इसे पता नहीं कि दुनिया कैसे चलती है।" और फिर उसे एक कोने में बिठाकर चाय पिलाई जाती, ताकि वह किसी और को 'ईमानदारी' का ज्ञान न दे पाए। बाबूजी कहते थे, "ईमानदारी तो एक बीमारी है, और इसका इलाज सिर्फ पैसा है।" और वे इस इलाज को बड़ी शिद्दत से करते थे। उनका मानना था कि गरीबी एक पाप है, और रिश्वत एक मोक्ष का मार्ग। वे अक्सर अपनी आत्मा से कहते थे, "मैं जो भी कर रहा हूँ, समाज के भले के लिए कर रहा हूँ, आखिर किसी को तो भ्रष्टाचार को जिंदा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो यह बेचारा कैसे चलेगा?" और इस तरह, बाबू सुखराम ने भ्रष्टाचार के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया, या यूँ कहूँ, गंदे अक्षरों में।
एक दिन, शहर में एक नया जज आया, नाम था जज कर्मठ। उनके नाम में 'कर्म' था, लेकिन उनके इरादों में 'अर्थ' था, यानी पैसा। वे अपनी ईमानदारी का ढोंग ऐसे रचते थे, मानो वे दूध के धुले हुए हों, जबकि उनका पूरा शरीर भ्रष्टाचार के दलदल में सराबोर था। वे अक्सर अदालत में बड़े-बड़े भाषण देते थे, "न्याय की कुर्सी पर बैठकर मैं कभी किसी गलत काम का साथ नहीं दूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े!" और फिर शाम को अपने बंगले पर बैठकर, वे उन 'गलत कामों' की लिस्ट बनाते थे, जिन्हें वे पैसों के लिए 'सही' कर सकते थे। उनकी पत्नी, श्रीमती अर्थलक्ष्मी, भी कोई कम नहीं थीं। वे अक्सर अपने पड़ोसियों से कहती थीं, "मेरे पति देव तो न्याय के देवता हैं, उन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता।" और फिर अपने पति से कहती थीं, "सुनो जी, उस केस में कितने पैसे मिले थे? मुझे एक नई साड़ी लेनी है।" जज साहब अपनी पत्नी की 'पवित्र' इच्छाओं को पूरा करने के लिए जी-जान से भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। उनका मानना था कि पत्नी की खुशी ही असली न्याय है। उनके घर में पैसों का अंबार लगा रहता था, मानो लक्ष्मी जी ने वहीं स्थायी निवास बना लिया हो। वे अक्सर अपने मित्रों से कहते थे, "मैं तो बस एक माध्यम हूँ, पैसा तो खुद ही मेरे पास आता है।" और यह कहते हुए उनकी आँखें चमक उठती थीं, जैसे किसी गरीब को लॉटरी लग गई हो। जज साहब की अदालत में एक अजीबोगरीब नियम था, जो भी केस उनके पास आता, वह हमेशा 'सही' हो जाता, बशर्ते सही दाम मिल जाए। लोग कहते थे, "जज साहब की अदालत में न्याय नहीं, कीमत मिलती है।" और यह बात पूरी तरह सच थी। एक बार एक चोर को पकड़ा गया, जिसने एक करोड़ की चोरी की थी। चोर ने जज साहब को पचास लाख दिए और जज साहब ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया, यह कहकर कि "यह तो निर्दोष है, इसे फँसाया गया है।" चोर ने बाहर आकर कहा, "वाह रे न्याय! पचास लाख में तो एक करोड़ की चोरी माफ हो गई।" जज साहब अक्सर कहते थे, "मैं न्याय की रक्षा कर रहा हूँ, आखिर अन्याय को भी तो जीने का अधिकार है।" और वे इस अधिकार का पालन बड़ी निष्ठा से करते थे। उनका मानना था कि कानून एक लचीली चीज है, जिसे पैसे से मोड़ा जा सकता है। वे अक्सर अपनी आत्मा से कहते थे, "मैं जो भी कर रहा हूँ, समाज में समानता लाने के लिए कर रहा हूँ, आखिर अमीर और गरीब दोनों को तो न्याय मिलना चाहिए, चाहे वह पैसे से ही क्यों न मिले।" और इस तरह, जज कर्मठ ने न्याय के इतिहास में अपना नाम 'अधर्मठ' के रूप में लिखवा लिया।
अब बात करते हैं हमारे कहानी के नायकों की, किरण और आलोक, जो बेचारे इस 'न्याय' के मकड़जाल में फँस गए थे। उनके पिताजी, बाबू धर्मनिष्ठ, एक सच्चे और सीधे-सादे आदमी थे, जो भूल से सरकारी दफ्तर में नौकरी कर रहे थे। उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक बार, किसी उच्च अधिकारी ने उनसे बीस रुपये की रिश्वत लेने को कहा, और बाबूजी ने साफ मना कर दिया। बस फिर क्या था, उन्हें तुरंत 'रिश्वत' लेने के आरोप में जेल भेज दिया गया। कमाल की बात तो यह थी कि रिश्वत लेने का आरोप उन पर लगा, जिन्होंने कभी रिश्वत ली ही नहीं, और जिन्होंने करोड़ों की रिश्वत ली, वे बाहर घूम रहे थे, न्याय का ढोंग रचते हुए। किरण और आलोक अनाथ हो गए थे, क्योंकि उनकी माँ का निधन पहले ही हो चुका था। उन्हें उनके मामा-मामी के पास छोड़ दिया गया था, जो अपनी दरियादिली का ढोंग ऐसे रचते थे, मानो वे साक्षात दानवीर कर्ण हों, जबकि वे तो भिखारी से भी बदतर थे, खासकर जब बात दया की आती थी। मामी हमेशा चिल्लाती रहती थी, "हाय रे मेरी किस्मत! कहाँ फँस गई मैं! इन अनाथ बच्चों को पालना पड़ रहा है।" और फिर उन्हें बासी रोटी देती, जबकि उनके अपने बच्चे शाही भोज का आनंद लेते। आलोक अक्सर रोता था, "दीदी, मामी ने फिर बासी रोटी दी। संजीव को हलवा मिला और हमें खुरचन।" किरण उसे चुप कराती, "चुप हो जा आलोक, पिताजी आ जाएँगे।" लेकिन पिताजी तो जेल में थे, और कब आएँगे, यह कोई नहीं जानता था। मामाजी भी कोई कम नहीं थे। वे अक्सर बच्चों को पीटते थे, और फिर कहते थे, "यह तो तुम्हारी भलाई के लिए है, ताकि तुम सीखो कि जीवन में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं।" और यह कहते हुए उनका हाथ और जोर से पड़ता था। एक दिन, आलोक ने गलती से एक गिलास तोड़ दिया, और मामाजी ने उसे ऐसे पीटा, मानो उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। किरण ने आलोक को गले लगाया और खुद भी रोने लगी। बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन वहाँ भी उनका हाल बुरा था। संजीव, जो मामा-मामी का बेटा था, हमेशा उन्हें चिढ़ाता था, "तुम्हारे पिताजी चोर हैं, तभी तो जेल में हैं।" किरण को गुस्सा आता, वह कहती, "संजीव झूठा है!" लेकिन उसकी अपनी आवाज में भी डर था। रात को किरण और आलोक सोते नहीं थे, वे बस एक-दूसरे को पकड़कर रोते रहते थे। उनके गाल आँसुओं से गीले रहते थे, और उनके दिल में एक ही सवाल था - "पिताजी कब आएँगे?" और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, सिवाय दर्द और पीड़ा के। वे हर दिन इस आशा में जीते थे कि शायद आज पिताजी आ जाएँगे, लेकिन हर दिन उनकी आशा टूट जाती थी। उनके जीवन में सुख का एक भी क्षण नहीं था, केवल दुख, अपमान और पीड़ा थी।
एक रात, जब शहर नींद की आगोश में था, किरण और आलोक जाग रहे थे। आलोक सुबक रहा था, उसकी छोटी सी देह काँप रही थी। "दीदी, पिताजी कब आएँगे? मुझे मामाजी ने मारा। संजीव ने कहा, हमारे पिताजी चोर हैं।" किरण ने उसे अपने आलिंगन में भर लिया। उसकी अपनी आँखें भी डबडबा गईं थीं, लेकिन उसने अपने आँसुओं को रोक लिया। वह एक 'शिशु-माँ' बन चुकी थी, जिसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्वता हासिल कर ली थी। "चुप हो जा आलोक, चुप हो जा। मामी आ जाएगी।" वे दोनों दबे पाँव सोए हुए मामा-मामी के कपड़ों की चमक देख रहे थे, जो अंधकार में भी सफेद दूध से धुले लग रहे थे, जैसे श्मशान में अग्नि के स्फुलिंग। किरण के नन्हे से दिल में कसक उठी। ये कपड़े तो चमक रहे हैं, लेकिन उनका दिल काला क्यों है? मामी की आवाज रात की चुप्पी को चीरती हुई आई, "क्या है, क्या है किरण, आलोक क्या है रे?... ओ हो! भाई से लाड़ लड़ाया जा रहा है। मैं कहती हूँ किरण, तू यहाँ क्यों आई?" मामी ने झल्लाकर कहा। मामा भी उठ बैठे, "क्या बात है? क्या हुआ?" मामी ने तुरंत जवाब दिया, "हुआ मेरा सिर। दोनों भागने की सलाह कर रहे हैं। अलमारी की चाबी तो है? रात ही पाँच सौ रुपए लाकर रखे हैं।" मामा के दिमाग में तुरंत पैसे का ख्याल आया। वे उठकर बच्चों के पास आ गए, जहाँ वे दोनों सहमे, सकपकाए, कबूतर की तरह आँखें बंद किए पड़े थे। मामी ने किरण को झटककर उठाया, "चल अपनी खाट पर। बाप तो आराम से जेल में जा बैठा, मुसीबत डाल गया मुझ पर।" मामा को संतोष हुआ कि पैसे नहीं निकले। उन्होंने अपनी ज्ञान की गंगा बहाई, "बहनोई साहब को रिश्वत लेने की सूझी और रिश्वत भी क्या थी, बीस रुपए की। वह भी लेनी नहीं आई। वहीं पकड़े गए।" मामी ने बीच में टोका, "इतनी बुद्धि होती तो क्या अब तक तीसरे दर्जे का क्लर्क बना रहता।" फिर मामा ने कहा, "और मजा यह कि जब मैंने कहा कि तीन सौ, चार सौ रुपए का प्रबंध कर दे, तुझे छुड़ाने का जिम्मा मेरा, तो सत्यवादी बन गया—'मैं रिश्वत नहीं दूँगा।' नहीं दूँगा तो ली क्यों थी?" यह सब सुन कर किरण और आलोक की नींद आँखों से उड़ गई थी। उनके गालों पर आँसू जमते जा रहे थे। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी - "पिताजी ने रिश्वत क्यों ली?" मामी और मामा की बातें उनके लिए रहस्यमयी पहेली थीं, जिन्हें वे सुलझा नहीं पा रहे थे। वे दोनों इस 'न्याय' और 'अन्याय' के खेल में मोहरे मात्र थे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं थी।
इसे भी पढ़ें: भगदड़ के बाद (व्यंग्य)
किरण के बंद आँखों के अंधेरे में पिता की मूर्ति और विशाल हो उठी। एक अधेड़ व्यक्ति, जिसकी आँखों में प्यार था, जिसकी वाणी में मिठास थी। पिता जो उन्हें नए स्कूल में भरती करवाते थे, जहाँ कोई मारता-झिड़कता नहीं था, जहाँ नाश्ता मिलता था, जहाँ वे तस्वीरें काटते थे, खिलौने बनाते थे। घर में पिता उनके लिए खाना बनाते थे, अच्छी-अच्छी किताबें लाते थे, फल लाते थे। उनकी माँ के मरने पर उन्होंने दूसरी शादी तक नहीं की थी। किरण ने यह सब पड़ोसियों से सुना था, जो उनके पिता की बड़ी तारीफ करते थे। उसने अपने कानों से पिता को यह कहते सुना था कि रिश्वत लेना पाप है। लेकिन फिर उन्होंने रिश्वत ली...क्यों ली...आखिर क्यों? पड़ोसिन कहती, "उसका खर्च बहुत था और आमदनी कम। वह बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता था, और तुम जानो, अच्छी शिक्षा बहुत महँगी है।" महँगी...महँगी थी तो उसने रिश्वत ली। महँगी होना क्या होता है, और अब पिता कैसे छूटेंगे? मामा कहते थे, "जज को रिश्वत देते तो छूट जाते। एक जज ने तीन हजार रुपए लेकर एक डाकू को छोड़ दिया था। एक आदमी जिसने एक औरत को मार डाला था, उसे भी जज ने छोड़ दिया था। पाँच हजार लिये थे।" पाँच हजार कितने होते हैं? सौ...हजार...दस हजार...लाख...ये कितने होते हैं। किरण के नन्हे से दिमाग में यह सब घूम रहा था। मामा कहते थे, "रिश्वत और भी तरह की भी होती है। एक प्रोफेसर ने एक लड़की को एम.ए. में अव्वल कर दिया था, क्योंकि वह खूबसूरत थी।" किरण ने सहसा दृष्टि उठाकर आसमान में देखा। तारे जगमगा रहे थे और आकाशगंगा का स्रोत धवल ज्योत्स्ना में लिपटा पड़ा था। उसने सोचा, यह सब कितना सुंदर है! क्या यहाँ भी रिश्वत चलती है? उसकी सुबकियाँ अब बिल्कुल बंद हो चुकी थीं और वह बड़ी गंभीरता से सुनी-सुनाई बातों को याद कर रही थी, पर समझ में उसकी कुछ नहीं आ रहा था... खूबसूरत होना भी क्या रिश्वत है? मामा कहते हैं कि गंजे हाकिम के पास खूबसूरत लड़की भेज दो और कुछ भी करवा लो... खूबसूरत लड़की और रुपया, रुपया और खूबसूरत लड़की... इन्हें लेकर जज और हाकिम काम क्यों कर देते हैं? क्यों...क्यों...और खूबसूरत लड़की वे क्या करते हैं? काम करवाते होंगे, पर काम तो सभी करते हैं... फिर खूबसूरत लड़की क्यों?... और उसके मामा बहुत से रुपए लाते हैं, पर लड़की कभी नहीं लाते! उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वह बस सोचती रही, इस 'रिश्वत' नाम की बला को, जो एक परिवार को तबाह कर सकती थी, और दूसरों को मालामाल।
सुबह पाँच बजे, मामी की कर्कश आवाज ने किरण की तंद्रा तोड़ी, "किरण, ओ किरण! अरी उठेगी नहीं? पाँच बजे हैं। कब से पुकार रही हूँ। दोनों भाई-बहन कुंभकर्ण से बाजी लगाकर सोते हैं। चल जल्दी। चौका-बासन कर। मैं आती हूँ।" किरण ने अंगड़ाई लेने का नाटक किया, फिर कुनमुनाती हुई उठी। जीने तक जाकर उसे कुछ याद आया, वह आलोक के पास गई और बड़े प्यार से कान से मुँह लगाकर उसे पुकारा। फिर उत्तर की प्रतीक्षा न करके उसे कौली में समेटकर नीचे लिए चली गई। दो घंटे बाद, मामी जब नीचे उतरी तो स्तब्ध रह गई। रसोईघर दूध में धोया गया था, लकदक-लकदक, मैल की कहीं छाया तक नहीं। बरतन चाँदी से चमचमा रहे थे। मामी ने अविश्वास से आँखें मलीं और ठगी सी बोली, "आज क्या बात है, किरण?" किरण ने सकपकाकर उत्तर दिया, "कुछ नहीं, मामी!" आलोक ने तुरंत कहा, "मामी! आज पिताजी आएँगे।" मामी ने अविश्वास और आशंका से ऐसे देखा कि आलोक सहमकर पीछे हट गया। कई क्षण तक उस स्तब्ध वातावरण में वे प्रस्तर-प्रतिमा बने रहे, फिर जैसे जागकर मामी बोली, "तो यह बात है। बाप के स्वागत के लिए रसोईघर सजाया गया है।" फिर एक बारगी बड़े जोर से हँसी, बोली, "पर रानीजी, अभी तो पूरे सात महीने बाकी हैं, सात महीने। बाह रे, वाह के लिए दिल में कितना दर्द है! इसका पासंग भी हमारे लिए होता तो..." किरण की काया एकाएक पीली पड़ गई। आग्नेय नेत्रों से आलोक की ओर देखती हुई वह वहाँ से चली गई। उस दृष्टि से आलोक सहम गया, पर उसे अपने अपराध का पता तब लगा जब यह हो चुका था। स्कूल जाते समय रास्ते में किरण ने इस अपराध के लिए आलोक को खूब डाँटा। इतना डाँटा कि वह रो पड़ा। रो पड़ा तो उसे छाती से लगाकर खुद भी रोने लगी। इस घटना ने एक बार फिर उन्हें याद दिलाया कि वे इस समाज में कितने अकेले थे, कितने असहाय थे। उनके पिता के जेल जाने से उनके जीवन में जो अंधकार आया था, वह कभी मिटने वाला नहीं था, बल्कि हर दिन गहराता ही जा रहा था।
उसी समय, शहर से बहुत दूर, एक सुसज्जित भवन में मुक्त अट्टहास गूँज रहा था। छोटे जज आज विशेष प्रसन्न थे। उनकी छोटी पुत्री श्रीमती शोभा को कमीशन ने सांस्कृतिक विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद के लिए चुन लिया था। मित्र बधाई देने आए हुए थे। यह उसी हर्ष का अट्टहास था। यद्यपि बाकायदा चाय-पार्टी का कोई प्रबंध नहीं था, तो भी मेज पर अच्छी भीड़भाड़ थी। अंग्रेज लोग चाय पीते समय बोलना पसंद नहीं करते थे, पर भारतवासी क्या अब भी उनके गुलाम हैं? वे लोग जोर-जोर से बातें कर रहे थे। शोभा ने चाय बनाते हुए कहा, "मुझे तो बिल्कुल आशा नहीं थी, पर सचिव साहब की कृपा को क्या कहूँ।" सचिव साहब बोले, "मेरी कृपा! आपको कोई 'न' तो कर दे? आपकी प्रतिभा..." डायरेक्टर कह उठे, "हाँ, इनकी प्रतिभा! सांस्कृतिक विभाग तो है ही नारी की प्रतिभा का क्षेत्र।" सचिव साहब के नेत्र जैसे विस्फारित हो आए, प्याले को ठक से मेज पर रखते हुए उन्होंने कहा, "क्या बात कही आपने! संस्कृति और नारी दोनों एक ही हैं। नाट्य, नृत्य, संगीत और कविता।" "और प्रचार?" "अरे, नारी से अधिक प्रचार कर पाया है कोई।" इसी समय बेयरे ने आकर सलाम झुकाई। तार आया था। खोलने पर जाना, छोटे जज साहब के बड़े बेटे की नियुक्ति इनकमटेक्स ऑफिसर के पद पर हो गई है। उसे मद्रास जाना होगा। "क्या, क्या" कहते हुए सब तार पर झपटे। हर्ष और भी मुखर हो उठा। छोटे जज ने अट्टहास करते हुए अपनी पत्नी से कहा, "देखो नमिता! मुझे पूरा विश्वास था, शर्मा मेरी बात नहीं टाल सकता। और मेरी बात भी क्या असल में वह तुम्हारा मुरीद है।" बात काटकर सचिव साहब बोले, "जी नहीं, यह न आप हैं और न श्रीमती नमिता। यह तो आपकी कौटुंबिक प्रतिभा है!" इस पर सबने स्वीकृति सूचक हर्ष-ध्वनि की। छोटे न्यायमूर्ति इसका प्रतिवाद कर पाते कि बेयरे ने आकर फिर सलाम किया। विस्मित से डायरेक्टर बोले, "इस बार इसकी नियुक्ति होनेवाली है?" बेयरे ने कहा, "दो बच्चे हुजूर से मिलने आए हैं।" "हमसे?" छोटे न्यायमूर्ति अचकचाकर बोले। "जी।" "किसके बच्चे हैं?" "जी, मालूम नहीं। भाई-बहन हैं। गरीब जान पड़ते हैं।" "अरे तो बेवकूफ, कुछ दे-दिवाकर लौटा दिया होता।" "बहुत कोशिश की, पर वे कुछ माँगते ही नहीं। बस आपसे मिलना माँगते हैं।" छोटे न्यायमूर्ति तेजी से उठे। मुख उनका विकृत हो आया, पर न जाने क्या सोचकर वे फिर बैठ गए। कहा, "आज खुशी का दिन है। यहीं ले आ।" यह विडंबना थी कि जहाँ एक ओर न्याय के नाम पर भ्रष्टाचार का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर न्याय की तलाश में मासूम बच्चे दर-दर भटक रहे थे।
दो क्षण बाद, बुरी तरह सहमे, सकपकाए जिन दो बच्चों ने वहाँ प्रवेश किया, वे किरण और आलोक थे। आँसुओं के दाग अभी गालों पर शेष थे। दृष्टि से भय झरा पड़ता था। एक साथ सबने उनको देखा और मदिरा के प्याले में मक्खी पड़ गई हो। छोटे न्यायमूर्ति ने पूछा, "कहाँ से आए हो?" "जी...जी..." किरण ने कहना चाहा, पर मुँह से शब्द नहीं निकले और बावजूद सबके आश्वासन के वे कई क्षण हतप्रभ, विमूढ, अपलक देखते ही रहे, बस देखते ही रहे। आखिर शोभा उठी। पास आकर बोली, "कितने प्यारे, कितने सुंदर बच्चे हैं!" इन शब्दों में न जाने क्या था! किरण को जैसे करंट छू गई। एक बारगी दृढ़ कंठ से बोल उठी, "आपने हमारे पिताजी को जेल भेजा है। आप उन्हें छोड़ दें।" आलोक ने उसी दृढ़ता से कहा, "हमारे पास पचास रुपए हैं। आपने तीन हजार लेकर एक डाकू को छोड़ा है।" किरण बोली, "लेकिन हमारे पिताजी डाकू नहीं हैं। महँगाई बढ़ गई थी। उन्होंने बस बीस रुपए की रिश्वत ली थी।" आलोक ने कहा, "रुपए थोड़े हों तो..." किरण बोली, "तो मैं एक-दो दिन आपके पास रह सकती हूँ।" आलोक ने कहा, "मेरी दीदी खूबसूरत है और आप खूबसूरत लड़कियों को लेकर काम कर देते हैं।" रटे हुए पार्ट की तरह एक के बाद एक जब वे दोनों इस प्रकार बोल रहे थे, तो न जाने हमारे कथाकार को क्या हुआ, वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे धरती सूर्य की चुंबक शक्ति से अलग हो रही है। लेकिन ऐसा होता तो क्या हम 'पुनश्च' लिखने को बाकी रहते? धरती अब भी उसी तरह घूम रही है। इस दृश्य ने एक पल के लिए जश्न के माहौल को खामोश कर दिया था। न्याय की कुर्सी पर बैठे वे लोग, जो पैसों के लिए न्याय बेचते थे, आज उन मासूम बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। उनके चेहरे पर डर और शर्म साफ दिख रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इन बच्चों को कैसे चुप कराया जाए, कैसे उनके सवालों का जवाब दिया जाए। बच्चों की मासूमियत ने उनके भ्रष्ट जीवन के सारे ढोंग को एक पल में तोड़ दिया था।
रात का अंधेरा गहरा रहा था, लेकिन किरण और आलोक की आँखों में नींद नहीं थी। वे वापस अपने मामा-मामी के घर आ गए थे, लेकिन उनके दिल में शांति नहीं थी। वे छोटे जज के सामने अपनी बात कहकर आए थे, लेकिन क्या इससे कुछ बदलेगा? उन्हें नहीं पता था। उनकी मासूम आँखों के सामने अभी भी वे चमकते हुए चेहरे घूम रहे थे, वे अट्टहास गूँज रहे थे, और वे ठंडे, बेजान शब्द। उन्हें लगा कि वे किसी ऐसे दलदल में फँस गए हैं, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। आलोक सुबक रहा था, "दीदी, पिताजी कब आएँगे? क्या वे कभी नहीं आएँगे?" किरण ने उसे अपने सीने से लगा लिया, उसकी आँखों से आँसू झर रहे थे। वह अब रो रही थी, खुलकर, बिना किसी रोक-टोक के। उसकी 'शिशु-माँ' की भूमिका टूट चुकी थी, और अब वह सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, जो अपने पिता को याद कर रही थी, जो न्याय और अन्याय के इस जटिल खेल को समझ नहीं पा रही थी। उन्हें लगा, जैसे वे इस विशाल दुनिया में अकेले हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। उनके मामा-मामी, जो उनके अभिभावक थे, वे भी उनके साथ नहीं थे, बल्कि उन्हें और दर्द दे रहे थे। उन्हें लगा कि उनका जीवन सिर्फ पीड़ा, अपमान और अकेलेपन से भरा है। उनके पिता, जो जेल में बंद थे, वे भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा कि वे इस दुनिया में बोझ हैं, जिनकी कोई जरूरत है। उन्हें लगा कि उनका जीवन सिर्फ पीड़ा, अपमान और अकेलेपन से भरा है। उनके पिता, जो जेल में बंद थे, वे भी उनकी मदद नहीं कर सकते थे। उन्हें लगा कि वे इस दुनिया में बोझ हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है। उनके दिल में एक अजीब सी कसक थी, एक ऐसा दर्द था, जो उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। उन्हें लगा कि वे मर जाना चाहते हैं, ताकि इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। यह वो पीड़ा थी, जो आत्मा को झकझोर देती है, यह वो अकेलापन था, जो इंसान को तोड़ देता है। उनके लिए अब कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। उनका जीवन एक ऐसा अंधकार था, जिससे कभी उजाला नहीं आने वाला था। और इसी दर्द, इसी अकेलेपन में, वे दोनों भाई-बहन एक-दूसरे को कसकर पकड़े, रात भर जागते रहे, और उनके आँसू उनके गालों पर जमते गए, जैसे बर्फ के कण। उनकी आह, जो उनके दिल से निकली थी, पूरे ब्रह्मांड में गूँज रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। यह वो त्रासदी थी, जो हर कोने में छिपी हुई थी, हर घर में, हर परिवार में। और कोई इसे देख नहीं पा रहा था, या शायद देखना नहीं चाहता था।
- डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा ‘उरतृप्त’,
(हिंदी अकादमी, मुंबई से सम्मानित नवयुवा व्यंग्यकार)
अन्य न्यूज़