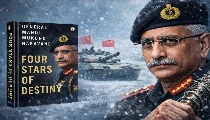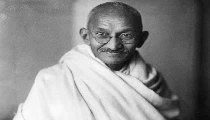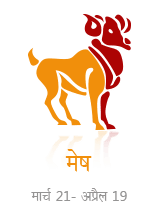Chai Par Sameeksha: Modi के 11 साल में Middle Class की गाड़ी बीच में ही अटकी रही या कुछ आगे बढ़ी?

मिडिल क्लास अक्सर सरकार से कोई मांग या शिकायत करने का समय नहीं निकाल पाता इसलिए कोई सरकार इनकी ओर ध्यान ही नहीं देती थी लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से निकाल कर मध्यम वर्ग में पहुँचाया और उनका जीवन आसान भी बनाया।
मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार बता रही है कि उसने गरीबों के लिए क्या किया और विपक्ष बता रहा है कि मोदी सरकार ने अमीरों के लिए क्या किया। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास यानि मध्यम वर्ग के लिए क्या किया। ये जो मिडिल क्लास है ये सिर्फ अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने में ही जुटा रहता है और अक्सर सरकार से कोई मांग या शिकायत करने का समय नहीं निकाल पाता इसलिए कोई सरकार इनकी ओर ध्यान ही नहीं देती थी लेकिन मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से निकाल कर मध्यम वर्ग में पहुँचाया और इस मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाने के लिए तमाम स्थायी उपाय भी किये।
देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब तक के कार्यकाल में भारत के मध्यम वर्ग ने खुद को राष्ट्र की प्रगति की कहानी के केंद्र में पाया है। उनकी आशाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को न केवल सुना गया है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से उन पर काम भी किया गया है। कर राहत से लेकर उनके हाथों में अधिक पैसा आने तक, पेंशन योजनाओं से लेकर बुढ़ापे में सुरक्षा का वादा करने तक, पिछले ग्यारह वर्षों में लाखों लोगों के जीवन को आसान, निष्पक्ष और अधिक सम्मानजनक बनाने के लिए लगातार और ईमानदार प्रयास किए गए हैं।
इसे भी पढ़ें: मोदी युग के 11 वर्ष और अजमेर की विकास यात्रा
मोदी सरकार ने लालफीताशाही को खत्म किया है, नियमों को सरल बनाया है और रोजमर्रा की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया है। चाहे टैक्स दाखिल करना हो, घर खरीदना हो, काम पर आना-जाना हो या दवाइयों का खर्च उठाना हो, चीजें सरल और अधिक सुलभ हो गई हैं। ये सुधारों का एक पैटर्न है जो आम नागरिकों की वास्तविक चिंताओं को दर्शाता है। इसमें विशेष बात है निरंतरता। साल दर साल, बजट दर बजट, कदम दर कदम, सरकार मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रही है। ऐसा करके, उसने न केवल उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान किया है, बल्कि उन्हें भारत के विकास के प्रमुख चालकों के रूप में भी मान्यता भी दी है। पिछले ग्यारह वर्षों में, सरकार ने मध्यम वर्ग के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने के लिए प्रतीकात्मक उपायों से आगे बढ़कर काम किया है। आयकर दरों को कम करने से लेकर रिटर्न को सरल बनाने तक, हर कदम नागरिकों को उनकी कमाई का ज़्यादा हिस्सा रखने देने के मूल विचार के साथ जुड़ा हुआ है।
हम आपको बता दें कि सबसे हालिया कर सुधार, विशेष रूप से केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए सुधार, इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि सरकार ने राष्ट्रीय विकास के स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर अपना भरोसा रखा है। चाहे वह शून्य कर के लिए आय सीमा बढ़ाना हो, सरल कर व्यवस्था शुरू करना हो या रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज़्यादा आसान बनाना हो, प्रयास निरंतर और केंद्रित रहे हैं। जो बात सबसे अलग है, वह सिर्फ़ सुधारों का पैमाना नहीं है, बल्कि ईमानदार, मेहनती करदाताओं के लिए निष्पक्षता और मान्यता की भावना है। पिछले ग्यारह वर्षों में, आयकर नीति ने लगातार सार्थक राहत प्रदान की है। सरकार ने छूट की सीमा बढ़ाई, मानक कटौती शुरू की, 2020 में सरलीकृत कर व्यवस्था शुरू की और कागजी कार्रवाई कम की। इन प्रयासों से करदाताओं का जीवन आसान हुआ है।
इसके अलावा, 2014 तक के वर्षों में, बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग के परिवारों को लगातार तनाव में रखा। 2009-10 और 2013-14 के बीच, मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में रही। भोजन और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुएँ लगातार महंगी होती गईं। घरेलू बजट पर दबाव पड़ा और बचत करना पहुंच से बाहर हो गया। 2004-05 से 2013-14 के दशक पर नज़र डालें तो औसत वार्षिक मुद्रास्फीति 8.2 प्रतिशत पर रही। मूल्य अस्थिरता की इस लंबी अवधि ने रोजमर्रा की जिंदगी को कठिन बना दिया और भविष्य की योजना बनाना अनिश्चित हो गया। मगर 2014 से चीजें बदलने लगीं। अगले ग्यारह सालों में महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाया गया। 2015-16 से 2024-25 तक महंगाई औसत दर गिरकर सिर्फ़ 5 प्रतिशत रह गई। यह अंतर सिर्फ़ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिखाई देता है। स्थिर कीमतों ने परिवारों को राहत दी। ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा किफ़ायती हो गईं और मासिक खर्चों की योजना बनाना आसान हो गया। यह बदलाव ठोस नीति, रिजर्व बैंक के साथ मज़बूत समन्वय और बेहतर आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन का नतीजा था। लंबे समय से बढ़ती कीमतों की मार झेल रहे मध्यम वर्ग को आखिरकार राहत मिली और अर्थव्यवस्था में उनका भरोसा फिर से लौटा।
इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करने के एक बड़े कदम के तौर पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंज़ूरी दी। यह योजना सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन सुनिश्चित करती है, जो कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों पर लागू होती है। कम सेवा अवधि वाले लोगों के लिए, पेंशन की गणना आनुपातिक रूप से की जाएगी, जिसमें न्यूनतम योग्यता अवधि 10 वर्ष होगी। 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद रिटायर होने पर न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, उनके परिवार को सुनिश्चित पेंशन के 60% के बराबर पेंशन मिलेगी। एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू हुई और इससे लगभग 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कई राज्य सरकारों ने भी इस मॉडल को अपनाया है, जिससे वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत 90 लाख से अधिक व्यक्तियों तक इसका कवरेज बढ़ा है।
साथ ही, पिछले ग्यारह वर्षों में, भारत के शहरी परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। किफायती आवास उन लोगों तक पहुँच गया है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बेहतर सड़कें, स्वच्छ हवा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएँ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के साथ शहर ज़्यादा रहने लायक बन गए हैं। मध्यम वर्ग के लिए, ये गरिमा और सुविधा लाए हैं। ये लाभ दीर्घकालिक दृष्टि, निरंतर वित्तपोषण और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम हैं। पहली बार घर खरीदने वालों से लेकर रोज़ाना मेट्रो से यात्रा करने वालों तक, करोड़ों नागरिकों ने अपने घरों, अपनी सड़कों और अपने आस-पड़ोस में बदलाव महसूस किया है। पिछले 11 सालों में शहरी परिवहन में सबसे बड़ी तेज़ी देखी गई। अब 29 शहरों में मेट्रो रेलें चल रही हैं या बन रही हैं। मई 2025 तक, भारत में 1,013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थीं, जो 2014 में सिर्फ़ 248 किलोमीटर थी। यानी सिर्फ़ ग्यारह साल में 763 किलोमीटर का इज़ाफ़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है।
इसके अलावा, 21 अक्टूबर 2016 को शुरू की गई उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। अपने छठे वर्ष में, उड़ान ने 625 मार्गों के माध्यम से 2 जल हवाई अड्डों और 15 हेलीपोर्ट सहित 90 हवाई अड्डों को जोड़ा है। 27 अप्रैल 2017 को शिमला से दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरी गई। तब से, 1.49 करोड़ से अधिक यात्रियों को कम लागत वाली क्षेत्रीय हवाई यात्रा का लाभ मिला है। भारत का हवाई अड्डा नेटवर्क 2014 में 74 हवाई अड्डों से बढ़कर 2024 में 159 हो गया है। वंचित क्षेत्रों में हवाई संपर्क का समर्थन करने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि के रूप में 4,023.37 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इस योजना ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार किया है और टियर 2 और टियर 3 शहरों में व्यापार को बढ़ावा दिया है, जिससे समावेशी क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला है।
इसके अलावा, घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने और आवास क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए, संसद ने 2016 में रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम पारित किया। यह रियल एस्टेट लेनदेन में जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आरईआरए के तहत, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एक नियामक प्राधिकरण स्थापित किया, जिसे पंजीकृत विकास के लिए परियोजना विवरण सूचीबद्ध करने वाले सार्वजनिक पोर्टल को बनाए रखने का काम सौंपा गया।
यही नहीं, भारत में स्वास्थ्य सेवा ने पिछले ग्यारह वर्षों में एक मौन लेकिन दूरगामी बदलाव देखा है। लक्षित सार्वजनिक योजनाओं और डिजिटल पहुंच के मिश्रण के माध्यम से, सरकार ने लाखों लोगों, खासकर मध्यम वर्ग के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुलभ बनाया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पताल में भर्ती से लेकर देश भर में उपलब्ध कम कीमत वाली दवाओं तक, आज लोगों के पास अपने स्वास्थ्य खर्चों पर बेहतर नियंत्रण है। इन योजनाओं का समर्थन करने वाली डिजिटल रीढ़ ने नामांकन, पहुँच और ट्रैकिंग को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। इस बदलाव ने मध्यम वर्ग को नौकरशाही की बाधाओं के बिना दवाओं पर बचत, समय पर उपचार और चिकित्सा सुरक्षा का लाभ उठाने का अवसर दिया है।
इसके अलावा, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में से एक बनकर उभरी है। 3 मई, 2025 तक, 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 40.84 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना ने 1,19,858 करोड़ रुपये मूल्य के 8.59 करोड़ लोगों को अस्पताल में भर्ती होने में सक्षम बनाया है, जिससे परिवारों को कर्ज में डाले बिना माध्यमिक और तृतीयक देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित हुई है।
इसके अलावा, पिछले ग्यारह वर्षों में, सरकार ने भारत के महत्वाकांक्षी मध्यम वर्ग के लिए कौशल और सीखने के परिदृश्य को फिर से परिभाषित किया है। रोजगार, समावेशिता और उद्योग संरेखण पर स्पष्ट ध्यान देने के साथ, कार्यक्रमों के एक विस्तृत नेटवर्क ने लाखों भारतीयों को नौकरी के लिए कौशल हासिल करने में मदद की है। 2014 में स्थापित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक महत्वपूर्ण जरूरत के जवाब के रूप में जो शुरू हुआ वह आज दुनिया में सबसे बड़े मानव पूंजी विकास प्रयासों में से एक बन गया है। अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से लेकर प्रशिक्षुता, सामुदायिक शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक, सरकार के दृष्टिकोण ने शहरी केंद्रों और ग्रामीण परिवारों को समान रूप से छुआ है, जिससे अवसर, स्थिरता और आशा मिली है।
इसके अलावा, 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) भारत में अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण की रीढ़ बन गई। 18 अप्रैल 2025 तक, इसने विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, आईटी और निर्माण जैसे क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण के माध्यम से 1.63 करोड़ से अधिक युवाओं को व्यावहारिक कौशल से लैस किया। इस योजना में समावेशिता पर जोर दिया गया, जिससे महिलाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों की बड़ी भागीदारी देखी गई। यह समय के साथ विकसित भी हुआ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेचैट्रॉनिक्स जैसे भविष्य के डोमेन पेश किए गए। पीएमकेवीवाई ने सुनिश्चित किया कि कौशल प्रशिक्षण एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि, अधिकार है, जिसे दूरदराज के गांवों में भी उपलब्ध कराया गया है।
इसके अलावा, पिछले ग्यारह वर्षों में, भारत में डिजिटल गवर्नेंस मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। सुलभ, कुशल और पारदर्शी डिजिटल सेवाओं की ओर सरकार के केंद्रित प्रयास ने नागरिकों के राज्य के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल दिया है। दस्तावेज़ों तक पहुँच से लेकर सेवा वितरण तक, वित्तीय समावेशन से लेकर कल्याण तक पहुँच में, डिजिटल उपकरणों ने लालफीताशाही को कम किया है, समय की बचत की है और घरों को सुविधाजनक बनाया है। मध्यम वर्ग को, विशेष रूप से, जल्दी सेवाओं के मिलने, कार्यालयों के कम चक्कर लगाने और कम कागजी कार्रवाई से लाभ हुआ है। आधार, डिजिलॉकर और उमंग जैसी प्रमुख पहलों ने न केवल सार्वजनिक सेवाओं को मोबाइल और कागज़ रहित बनाया है, बल्कि सरकारी प्रणालियों में विश्वास भी बढ़ाया है।
इसके अलावा, 2009 में शुरू किया गया आधार दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम बन गया है। मार्च 2014 तक 61.01 करोड़ आधार नंबर जारी किए जा चुके थे, जो अप्रैल 2025 के अंत तक बढ़कर 141.88 करोड़ से ज़्यादा हो गए। अब तक आधार ने 150 बिलियन से ज़्यादा प्रमाणीकरण लेन-देन को सक्षम बनाया है। इसका डिज़ाइन सुनिश्चित करता है कि लाभ डुप्लिकेट और धोखाधड़ी को हटाकर इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुँचें। देखा जाये तो मध्यम वर्ग ने बैंकिंग, पेंशन, स्कूल में दाखिले और ऑनलाइन सेवाओं तक आसान पहुँच देखी है, जो सभी सहज आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से संभव हुआ है। इसका बढ़ता उपयोग एक सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल पहचान प्रणाली में जनता के भरोसे को दर्शाता है।
बहरहाल, पिछले ग्यारह वर्षों में, सरकार ने सार्थक तरीकों से मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। शुरू की गई नीतियों और सुधारों ने न केवल रोज़मर्रा की चुनौतियों को कम किया है, बल्कि वित्तीय सुरक्षा, आवास, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास को भी मज़बूत किया है। ये बदलाव भारत की विकास कहानी में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका की स्पष्ट समझ को दर्शाते हैं। निष्पक्षता, सरलता और पहुँच पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार ने सुनिश्चित किया है कि लाखों मध्यम आय वाले परिवार भविष्य का सामना आत्मविश्वास के साथ करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हों। इस निरंतर और विचारशील दृष्टिकोण ने जीवन को बदल दिया है और निरंतर प्रगति के लिए एक मजबूत नींव रखी है।
अन्य न्यूज़