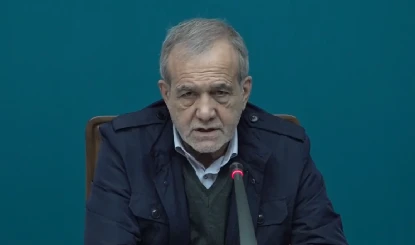अमेरिकी मनमर्जी को रोकने के लिए विश्व को एक होना पड़ेगा

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 और 1971 के युद्धों में अमेरिका में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, अमेरिकी सेनाओं और सरकार ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया और भारत का विरोध किया। साल 2024 में हुए बांग्लादेश में विद्रोह और शेख हसीना के तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी एजेंसियों के हाथ को लेकर संदेह जताया जाता है।
1995 में एक फिल्म आई थी, गैंबलर। गोविंदा-शिल्पा शेट्टी अभिनीत इस फिल्म का एक गाना उन दिनों बेहद मशहूर हुआ था, “मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी” निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप ने ये गाना नहीं सुना होगा, लेकिन उन्होंने हाल ही में न्यूयार्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जो कहा है, उसका भावार्थ कुछ यही निकलता है। उन्होंने कहा है, “सिर्फ मेरा दिमाग ही मुझे रोक सकता है। मेरी अपनी नैतिकता और अपना दिमाग। यहीं वे चीज़ें हैं, जो मुझे रोक सकती हैं। मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं है और न ही इसकी ज़रूरत।”
तीन जनवरी को वेनेजुएला में की गई अमेरिकी कार्रवाई के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप का इन शब्दों का प्रयोग करना दुनिया के लिए निश्चित तौर पर डरावना है। ट्रंप और उनकी सोच पारंपरिक लोकतांत्रिक मुखौटाबाज राजनीति से अलग है, लिहाजा वे खुलकर ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सुपर पावर के रूप में स्थापित होने के बाद से ही अमेरिका की सोच और कार्यशैली ऐसी ही रही है। अमेरिका की सत्ता में दो ही पार्टियों का वर्चस्व है। चाहे रिपब्लिकन पार्टी हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के राष्ट्रपतियों की कार्यशैली कम से कम विदेश मामलों में एक जैसी ही रही है। ट्रंप खुलकर ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति और नीयत का हवाला देते हैं, लेकिन दूसरे राष्ट्रपति ऐसा कहने से बचते रहे हैं। हां, उनके भी कदम हमेशा ऐसा ही रहे हैं। अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई हो, खाड़ी युद्ध हो, सूडान स्थित अमेरिकी दूतावास पर आतंकी हमले के बाद अमेरिकी कार्रवाई हो, वियतनाम का युद्ध हो, ईरान पर कार्रवाई हो, हर जगह अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई करता रहा है। बेशक उसे कई बार मुंह की खानी पड़ी है। हाल ही में ट्रंप के पूर्व राष्ट्रपति रहे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडन की सेनाएं अफगानिस्तान छोड़कर भाग खड़ी हुईं। वियतनाम का युद्ध लंबा चला था। इसे शुरू किया था डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने और जब अमेरिका वियतनाम युद्ध में फंसता नजर आया तो रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति रहे रिचर्ड निक्सन ने सेनाओं की वापसी कराई।
इसे भी पढ़ें: Donald Trump ने ईरानी अधिकारियों के साथ बैठकें रद्द कर प्रदर्शनकारियों से कहा, ‘मदद भेजी जा रही है’
कुवैत पर जब इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन ने हमला किया, तब जार्ज बुश सीनियर राष्ट्रपति थे। अमेरिका में एक धारणा रही है कि कुवैत पर कब्जे की कार्रवाई इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी इशारे पर ही की थी। लेकिन जब मामला उल्टा पड़ गया तो जॉर्ज बुश सीनियर ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्तावों की आड़ में ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के साथ गठबंधन करके सैनिक कार्रवाई शुरू की। 1990 में अमेरिकी कार्रवाई के चलते इराकी गार्ड को कुवैत को खाली करना पड़ा। इसके बाद इराक अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया। वैसे लंबे समय तक चले ईरान-इराक युद्ध के पीछे भी अमेरिकी हित काम कर रहे थे। तब दुनिया दो धुवीय थी। एक तरफ सोवियत संघ की अगुआई में विश्व का एक बड़ा हिस्सा काम कर रहा था तो दूसरी ओर अमेरिकी अगुआई में ज्यादातर नाटो देश सक्रिय थे। अफगानिस्तान में जब पिछली सदी के अस्सी के दशक में सोवियत सेनाएं घुसीं, तब सोवियत संघ को काबू करने के लिए अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान का उपयोग किया और एक तरह से पाकिस्तान को अपना अघोषित उपनिवेश बना लिया।
भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 और 1971 के युद्धों में अमेरिका में चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, अमेरिकी सेनाओं और सरकार ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दिया और भारत का विरोध किया। साल 2024 में हुए बांग्लादेश में विद्रोह और शेख हसीना के तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी एजेंसियों के हाथ को लेकर संदेह जताया जाता है। साल 2010 के दिसंबर में ट्यूनिशिया में शुरू हुई पिंक क्रांति, जिसे अरब क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, की बुनियाद पर अरब देशों में कार्रवाई करने और तख्तापलट के पीछे भी अमेरिकी एजेंसियों के सहयोग को देखा जाता है। अमेरिकी एजेंसियों की ही शह पर लीबिया से गद्दाफी की विदाई हुई, सीरिया अब भी जल रहा है। निश्चित तौर पर अमेरिकी प्रतिकार में शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष काम करता था, अब दुनिया की दूसरे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बन चुका चीन कर रहा है। हाल ही में वेनेजुएला के जिन मादुरो की सत्ता को अमेरिकी सेनाओं ने पलट दिया, उन्हें चीन का खुला समर्थन मिल रहा था। शीत युद्ध के दिनों में सोवियत संघ और उसकी सेना ऐसे हालात में अमेरिकी सेनाओं का परोक्ष विरोध करती थी, वैसा चीन नहीं कर पाया।
कह सकते हैं कि अमेरिका में हर सत्ता ने वैश्विक ताकत क्रम में खुद को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए अपने हिसाब से दादागिरी दिखाई है। कभी यह दादागिरी अमेरिकी हितों के नाम पर हुई तो कभी दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर। कहने के लिए अमेरिका लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरूआ बनता है, लेकिन अमेरिकी हितों, कारोबारियों और हथियार लॉबी के हित में अक्सर वह गैर लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई करता है। दुनिया का आधुनिक इतिहास इससे भरा पड़ा है। वेनेजुएला इसका ताजा उदाहरण है। ट्रंप जिन अंतरराष्ट्रीय कानूनों को अपने हिसाब से मानने या न मानने की बात कर रहे हैं, दरअसल उन्हें बनाने और संशोधित करने में सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका का ही रहा है। विश्व में जब भी कहीं वेनेजुएला जैसी घटना होती है, तब जिनेवा समझौते और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का बहुत जिक्र होता है। दरअसल उन्नीसवीं सदी के मध्य तक दुनिया में होने वाले युद्धों के लिए युद्धबंदियों और सैनिकों और युद्धग्रस्त देशों के लोगों को लेकर शत्रु देशों की ओर से की जाने वाली अमानवीय कार्रवाई को रोकने के लिए ना तो कोई कानून था और इसे लेकर कोई प्रयास हुआ था। साल 1864 में पहली बार युद्ध के वक्त घायलों की मदद युद्धरत देशों के बीच बातचीत के लिए रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट ने कोशिश की। यही कोशिश पहले जेनेवा समझौते के रूप में सामने आई। इस दौरान युद्धरत देशों, उनके नागरिकों, सैनिकों आदि के मानवीय अधिकारों की रक्षा करने को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं। इसके तहत कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परिकल्पना की गई और युद्ध के प्रभाव को सीमित करने और युद्धबंदियों के अधिकारों के संरक्षण की कोशिश शुरू हुई। जेनेवा में आखिरी समझौता 1949 में हुआ। जिनेवा कन्वेंशन का मकसद युद्ध के वक्त मानवीय मूल्यों को बनाए रखने के लिये कानून तैयार करना है। 1949 के समझौते में शामिल दो प्रोटोकॉल 1977 में जोड़े गए। आज तकरीबन पूरी दुनिया ने इस पर हस्ताक्षर किया है। इस लिहाज से जेनेवा समझौते को सभी देश मानते हैं। जेनेवा समझौते के अनुसार हर देश की अपनी संप्रभुता है और उसकी रक्षा ना सिर्फ युद्ध बल्कि शांति काल में भी होती है। यानी उसके नियम और कानून युद्ध, शांति और संकट काल, हर वक्त लागू होते हैं। इस संदर्भ में देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना कि उनकी अपनी नैतिकता ही उन्हें किसी भी कार्रवाई से रोक सकती है। ट्रंप ने यहां तक कहा है कि जहां उन्हें लगेगा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय कानून मानना चाहिए, वहां तो उसे वे मान लेंगे और जहां नहीं लगेगा, वहां नहीं मानेंगे।
अमेरिकी दादागिरी के इतिहास में ट्रंप का यह बयान दुनिया की सोच से आगे है। चीन, ब्राजील और भारत के खिलाफ वे टैरिफ युद्ध चला ही रहे हैं, रूस से तेल खरीदने के आरोप की आड़ में वे तीनों देशों पर अब 25 प्रतिशत की बजाय पांच सौ प्रतिशत टैरिफ थोपने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप की जैसी फितरत है, उसकी वजह से उनसे कोई सकारात्मक उम्मीद रखना बेमानी ही है। भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रोकवाने को लेकर उनका कल्पित दावा हो या फिर ग्रीनलैंड, कोलंबिया, ईरान, मैक्सिको और क्यूबा को लेकर दी गई धमकी, सभी अमेरिकी दादागिरी का ही उदाहरण हैं। माना जा रहा है कि वे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं। ट्रंप पहले ही कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कर चुके हैं और इस तरह अपने पड़ोसियों और यूरोप के अपने पारंपरिक सहयोगियो को ना सिर्फ आशंकित, बल्कि नाराज भी कर चुके हैं।
अमेरिकी दादागिरी पूरी दुनिया देखती और समझती रही है। लेकिन एक साथ इतने मोर्चे खोल देने की ट्रंप की नीति के खिलाफ अमेरिका में ही आवाजें उठने लगी हैं। पूर्व अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कहना कि वेनेजुएला में की गई कार्रवाई की जरूरत नहीं थी और इससे अमेरिका को लेकर संघर्ष बढ़ेगा, एक तरह से अमेरिका की बढ़ती चुनौतियों का ही संकेत देता है। ट्रंप की मनमानी नहीं रूकी, अमेरिकी दादागिरी का ऐसा ही दौर उन्होंने जारी रखा तो आने वाले दिन दुनिया के लिए भले ही चुनौतीपूर्ण होंगे,अमेरिका भी कई तरह की चुनौतियों और वैश्विक प्रतिरोध को झेलने के लिए अभिशप्त हो जाएगा। शांति की चाहत रखने वाली दुनिया को अमेरिकी मनमर्जी पर कहीं न कहीं रोक तो लगानी ही होगी।
-उमेश चतुर्वेदी
लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं
अन्य न्यूज़