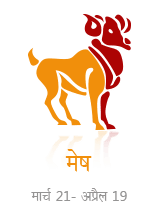बंटवारे का फार्मूला नेहरू और सरदार पटेल ने स्वीकारा था

बंटवारे का फार्मूला नेहरू और पटेल ने स्वीकार किया था, महात्मा गांधी ने नहीं। जब माउंटबेटन ने बंटवारे का फार्मूला तैयार कर लिया तो उन्होंने पहले महात्मा गांधी को बुलाया। गांधी ''''बंटवारा'''' शब्द सुनना नहीं चाहते थे और वह कमरे से बाहर निकल गए।
अंग्रेज इसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं कि जब उन्हें जर्बदस्ती या किसी और वजह से अपना उपनिवेश छोड़ने को मजबूर किया गया है तो उसकी स्थिति गड़बड़ करके ही वे उसे छोड़ते हैं। उन्होंने एक तरीका यह अपनाया है कि उस देश को बांट दिया है जिस पर उनका शासन था। उन्होंने यही आयरलैंड, फिलिस्तीन−इजरायल और बेशक, भारत में किया।
यह अगस्त, 2016 का का मध्य है और मैं लार्ड रेडक्लिफ, जिन्होंने भारत को दो देश− भारत और पाकिस्तान, में बांटने वाली रेखा खींची थी, से अपनी बातचीत को याद करता हूं। अंतिम वायसराय माउंटबेटन ने उन्हें ब्रिटेन के वकील−समुदाय से चुना था और उपमहाद्वीप को बांटने के लिए हवाई उन्हें हवाई जहाज से भारत लाया गया था। इसके पहले, रेडक्लिफ ने कभी भारत में पैर नहीं रखा था और न वह इस देश के बारे में ज्यादा जानते थे। रेडक्लिफ ने मुझे बताया कि माउंटबेटन ने उन्हें यह बताते हुए कि वह क्या चाहते थे, यह चेतावनी भी दी थी कि यह काम कठिन है और वह इसे नहीं भी कर पाएं। माउंटबेटन ने उन्हें 40 हजार रुपए देने की पेशकश की जो उस समय के लिए काफी बड़ा धन था। जैसा कि उन्होंने बताया कि उन्हें आखिरकार जिस चीज ने लुभाया वह था दो नए देश पैदा करने की जिम्मेदारी जो उनके कंधे पर डाली गई थी।
लंदन के एक नामी वकील के लिए रातोंरात अर्न्तराष्ट्रीय राजनेता बन जाने का विचार इतना आकर्षक था जिसे ठुकराया नहीं जा सकता था। रेडक्लिफ ने जिलों के मानचित्र मांगे, लेकिन एक भी उपलब्ध नहीं था। उन्हें जो कुछ कुछ मिला वह साधारण नक्शा था जो आफिस और शिक्षण संस्थानों की दीवारों पर टंगा रहता था।
रेडक्लिफ ने उसके आधार पर गणना की और एक अस्थायी रेखा मानचित्र पर ही खींच दी। उन्होंने मुझे बताया कि जिस आधार पर उन्होंने रेखा खींची थी उस पर लाहौर भारत को दिया। फिर उन्हें लगा कि वह पकिस्तान को एक महत्वपूर्ण शहर से वंचित कर देंगे। इसलिए, इसे ध्यान में रखते हुए लाहौर पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दिया। इस धरोहर को गंवाने के लिए उस समय के पूरबी पंजाब के लोगों ने उन्हें आज तक माफ नहीं किया है।
रेडक्लिफ ने चालीस हजार रूपए की अपनी फीस, जो वायसराय ने उन्हें देने का वायदा किया था, कभी नहीं ली क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि पलायन में जान गंवाने वाले दस लाख लोगों के लहू का बोझ उनके जमीर पर था। बंटवारे के बाद उन्होंने भारत का दौरा भी नहीं किया। लंदन में उनकी मौत हुई ओर भारतीय समाचार पत्रों ने यह खबर लंदन के द टाइम्स से ली। यह वही आदमी थे जिन्होंने दो मुल्कों का गठन किया था, लेकिन उन्हें कभी कोई सम्मान नहीं मिला। उन्हें आखिरकार अन्तरराष्ट्रीय राजनेता का दर्जा भी नहीं दिया गया।
कई साल बाद, पाकिस्तान के निर्माता कायदे−आजम मोहम्मद अली जिन्ना से उनके नौ सैनिक सहायक, जिसने बंटवारे में अपना माता−पिता खो दिया था, ने गुस्से में सवाल किया कि ''क्या पाकिस्तान हासिल करने लायक कोई अच्छी चीज थी?'' बूढ़े जिन्ना कुछ देर के लिए खामोश रहे और फिर उन्होंने जवाब दिया, ''नौजवान मुझे नहीं पता, यह सिर्फ भावी पीढी ही बताएगी।''
शायद, अभी कोई फैसला सुनाना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक चीज तो साफ है कि कायदे−आजम ने दो देशों को बांटने वाली रेखा धर्म के आधार पर खींची थी। यह एक विडंबना ही है क्योंकि जिन्ना ने कभी इसकी परवाह नहीं की वह क्या खाते हैं या क्या पीते हैं। यहां तक कि उन्होंने उर्दू को सरकारी भाषा बनाया, लेकिन वह खुद इसके कुछ शब्द रूक−रूक कर बोल पाते थे।
जब घटनाएं इस तरह तेजी से बढ़ रही थीं कि बंटवारे के अलावा कोई उपाय सामने नहीं रह गया था, महात्मा गांधी ने जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल को सलाह दी थी कि वे दोनों जिन्ना के सामने संयुक्त भारत के प्रधानमंत्री पद का आफर रखें। दोनों भयभीत हो गए क्योंकि दोनों ने अनेक सालों से इस पद पर अपनी नजरे टिका रखी थीं। इससे यही जाहिर होता है कि इसके बावजूद कि वे स्वतंत्रता आंदोलन की आग में तपे थे, लेकिन पद के लालच से ऊपर नहीं उठ पाए थे।
वास्तव में, बंटवारे का फार्मूला नेहरू और पटेल ने स्वीकार किया था, महात्मा गांधी ने नहीं। जब माउंटबेटन ने बंटवारे का फार्मूला तैयार कर लिया तो उन्होंने पहले महात्मा गांधी को बुलाया। गांधी ''बंटवारा'' शब्द सुनना नहीं चाहते थे और वह कमरे से बाहर निकल गए जब माउंटबेटन ने इसका नाम लिया। लेकिन पटेल और नेहरू ने बंटवारा स्वीकार कर लिया और खुद को समझा लिया कि उनकी जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं और देश का निर्माण करना है तो उन्हें माउंटबेटन की पेशकश स्वीकार कर लेनी चाहिए।
लेकिन जिन्हें बहुत ज्यादा दानव के रूप में चित्रित किया गया वह जिन्ना उस पाकिस्तान से खुश नहीं थे जो उन्हें मिला था। वह उसे ''कीड़े से कुतरा हुआ'' पाकिस्तान कहते थे क्योंकि उनके सपनों का पाकिस्तान कम से कम पेशावर से दिल्ली तक फैला हुआ होता। लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। अंग्रेजों ने उनके सामने जो पेशकश की थी वह इतनी ही थी। निश्चित तौर वह इतने नाराज थे कि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के कहने से माउंटबेटन ने उन्हें दो नए स्वतंत्र देशों के बीच कोई कड़ी रखने की सलाह दी तो जिन्ना का जवाब था, ''मैं उन (भारतीयों) पर विश्वास नहीं करता।'' जिन्ना ने माउंटबेटन को दोनों देशों का साझा गर्वनर जनरल बनाने का सुझाव भी स्वीकार नहीं किया।
कुछ लोग आज तक मानते हैं कि जिन्ना एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होते और इस तरह भारत भी एक रह जाता। पाकिस्तान एक ही व्यक्ति का शो था, इसलिए उस देश का विचार उन्हीं के साथ खत्म हो जाता। उस समय तक किसी को पता नहीं था कि जिन्ना को घातक कैंसर था। यह संदेह किया जाता है कि ब्रिटिश जानते थे और उन्हें सिर्फ कुछ समय तक इंतजार करना था− जिन्ना के दृश्य से गायब होने का। नेहरू की यह भविष्यवाणी कि 'पाकिस्तान ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा' का संबंध जिन्ना की छिपी बीमारी से नहीं था। उनके और कांग्रेस के शीर्ष के नेताओं का विचार था कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से टिकने लायक नहीं है।
नेहरू या कांग्रेस यह कभी जान नहीं पाए कि विंस्टन चर्चिल ने जिन्ना से वायदा किया था कि वह जिन्ना के सफल होने और पाकिस्तान का बनना सुनिश्चित करेंगे। चर्चिल को हिंदुओं से पागलपन की हद तक नफरत थी और उन्होंने कहा था कि वह इस अनेक जुबान वाले धर्म को समझ नहीं पाए। इसकी तुलना में इस्लाम कितना सरल और आसानी से समझने लायक है। उनके दिमाग में सामरिक मामले भी थे। पाकिस्तान भौगोलिक रूप से ऐसी जगह पर था कि वह एक तरफ तेल−संपन्न इस्लामिक दुनिया और दूसरी तरफ विशाल सोवियत यूनियन का द्वार खोलता था। एक कृतज्ञ असामी, पाकिस्तान का आकर्षण काबू पाने लायक नहीं था।
अनेक सालों बाद, जब मैं लंदन में रेडक्लिफ से मिला तो वह ब्रांड स्ट्रीट के संपन्न इलाके के एक फ्लैट में रहते थे। इसलिए मेरे लिए यह सोचना स्वाभाविक था कि कि उनके इर्द−गिर्द कुछ नौकर होंगे। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने खुद ही दरवाजा खोला और चाय बनाने के लिए खुद ही केतली लगाई। वह पाकिस्तान और अपनी जिम्मेदारी के बारे में बात करने में हिचकते थे। लेकिन जब मैं आमने−सामने था तो उन्हें जवाब देना पड़ा। उनके चेहरे पर हर जगह अफसोस लिखा था और वह ऐसा आदमी लगे जिसे महसूस हो रहा था कि बंटवारे के समय हुई हत्याएं उनकी जमीर पर बोझ बनी हुई थीं।
- कुलदीप नैय्यर
अन्य न्यूज़