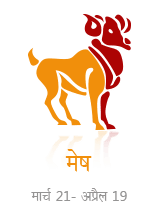ताकि बची रहे सांस्कृतिक बहुलता

यहां सवाल उठ सकता है कि भाषाओं को लेकर ऐसी बातों का संदर्भ क्या है? दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को ने भाषाओं को लेकर जो ताजा रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा गया है कि हर दो हफ्ते बाद दुनिया की एक भाषा मर रही है।
बीसवीं सदी के भाषा दार्शनिकों में लुडविग विट्गेंश्टाइन का नाम गंभीरता से लिया जाता है। लुडविग ने भाषा को लेकर अनोखी बात कही है, ‘मेरी भाषा की सीमा का अर्थ है, मेरी दुनिया की चौहद्दी।’ इसका साफ मतलब यह है कि हर व्यक्ति की अपनी भाषा दरअसल उसकी दुनिया होती है। ऐसी दुनिया, जिसमें सिर्फ भूगोल ही शामिल नहीं है, इतिहास भी है और संस्कृति भी, जिसमें परंपरा भी शामिल है और सदियों का अपना एक्सक्लूसिव ज्ञान भी। जिस तरह नदियां अपने उद्गम और अपने प्रवाह वाले इलाकों की पूरी संस्कृति और पर्यावरण के अथाह गुणों को खुद में समोए रहती हैं, भाषाएं भी नदी की भांति ही अपनी परंपरा, अपनी सोच, अपने दर्शन, अपने भूगोल और अपने इतिहास के साथ ही समूची संस्कृति को लेकर प्रवाहित होती रही हैं।
यहां सवाल उठ सकता है कि भाषाओं को लेकर ऐसी बातों का संदर्भ क्या है? दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन यूनेस्को ने भाषाओं को लेकर जो ताजा रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा गया है कि हर दो हफ्ते बाद दुनिया की एक भाषा मर रही है। यूनेस्को के अनुसार, पहले जहां हर तीन महीने के अंतराल पर एक भाषा की मौत की खबर आती थी, वहीं साल 2019 के बाद इस गति में तेजी आई है। यूनेस्को के मुताबिक, इस दर से हर साल दुनिया से करीब नौ भाषाओं का अस्तित्व खत्म होते जा रहा है। साफ है कि अगर एक भाषा मर रही है तो दरअसल उस भाषा की अपनी विशिष्ट संस्कृति, उसकी अपनी सोच और उसका अपना परिवेशबोध मर रहा है। इन अर्थों में देखें तो भाषाओं का इस तरह मरते जाना दरअसल संस्कृतियों के बहुलवादी स्वरूप का संकुचित होते जाना है।
इसे भी पढ़ें: सांस्कृतिक परम्पराओं के चलते पूरे विश्व में अपना विशेष स्थान बनाता भारत
यूनेस्को के अनुसार साल एक हजार ईस्वी तक दुनियाभर में नौ हजार से कुछ ज्यादा भाषाएं अस्तित्व में थीं। जिनकी संख्या घटते-घटते आज सात हजार के आसपास सिमट गई है। यूनेस्को को आशंका है कि भाषाओं के मरने की यही दर बनी रही तो 21वीं सदी के अंत तक दुनियाभर की करीब तीन हजार भाषाओं का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। भाषाओं के जानकारों के अनुसार, यूनेस्को का यह आकलन उम्मीदों से भरा है। जबकि पश्चिम के कई भाषा और मानवशास्त्री मानते हैं कि अगर भाषाओं के मरने की गति ऐसी ही रही तो साल 2200 ईस्वी तक दुनियाभर में महज 100 भाषाएं ही जीवित रह पाएंगी। भाषाओं के लुप्त होने को लेकर भारत में एक अवधारणा यह है कि जो भाषा क्लिष्ट या कठिन होती जाती है, वह लोकव्यवहार में खत्म होते जाती है। संस्कृत भाषा के बारे में नहीं कह सकते कि वह खत्म हो चुकी है, लेकिन उसका चलन घट गया है। एक खास धारा की वैचारिकी और भाषा दार्शनिक संस्कृत के चलन से बाहर होने के लिए उसके गंभीर होते जाने का उदाहरण देते हुए भाषाओं के लुप्त होने का सिद्धांत गढ़ते रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच भाषाएं सिर्फ इसी वजह से खत्म हो रही हैं कि वे क्लिष्ट या कठिन होती जा रही हैं? आधुनिक संदर्भों में देखें तो यह तर्क सही नहीं लगता। अंग्रेजी को ही लीजिए। कठिन अंग्रेजी बोलना शान का प्रतीक माना जाता है। इस लिहाज से तो उसे भी चलन से दूर होना चाहिए था। लेकिन उलटे वह बढ़ रही है।
आधुनिक विश्व में सबसे बेहतरीन व्यवस्था लोकतंत्र को माना जा रहा है। लेकिन यह लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक संदर्भों तक ही सिमटता जा रहा है। विश्व ग्राम में बदली दुनिया में हर देश में एकरूपता बढ़ती जा रही है। संस्कृतियां और उनकी अपनी विशिष्ट परंपराएं रोजाना के व्यवहार का विषय नहीं रहीं। उदारीकरण और वैश्वीकरण की वजह से पूरी दुनिया तकरीबन एक तरह से खानपान, एक तरह के पहनावे और एक तरह की भाषा की ओर आकर्षित होती जा रही है। पश्चिमी सभ्यता और उसका सलीका ही मानक बनते जा रहे हैं। इस लिहाज दुनियाभर की बोलियों में भी एकरूपता कभी सायासिक, तो कभी अनायास ही होती जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में छोटे समुदायों की भाषाएं लगातार किनारे होते जा रही हैं। चूंकि रोजी और रोजगार के लिए छोटे समुदायों की भाषाएं सहयोगी नहीं रह पाई हैं तो उनका चलन रोजाना की जिंदगी से कम होता जा रहा है और भाषाएं मर रही हैं। इसमें हर देश की अपनी केंद्रीय भाषा जहां केंद्रीय भूमिका में हैं, वहीं उसके देसज रूप लगातार या तो कमजोर हुए हैं या फिर लुप्त हो रहे हैं। कथित आधुनिक सोच इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दे रही है। भारत में अंग्रेजी इस आधुनिकता की वाहक है। इसी तरह कुछ प्रमुख भाषाएं अपने-अपने क्षेत्रों में आधुनिकता का केंद्रीय तत्व बन चुकी हैं।
इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ऐसी भाषाएं हैं, जो इतने कम लोगों द्वारा बोली जाती हैं कि निकट भविष्य में उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यूनेस्को की रिपोर्ट ‘एटलस-लुप्तप्राय भाषाएं’ के अनुसार भारत में तीन ऐसी भाषाएं हैं, जिनके अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ है। इसमें पहले नंबर पर कर्नाटक की कोरगा है, जिसे बोलने वालों की संख्या महज सोलह हजार ही है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सिरमौरी भाषा है, जिसे महज 31 हजार लोग ही बोलते हैं। इस सूची में तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ की पारजी भाषा है, जिसे सिर्फ पचास हजार लोग बोल रहे हैं। जाहिर है कि इन भाषाओं के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ है। एकीकरण के दौर में रोहिंग्या लोगों की भाषा हनीफी पर मरने के कगार पर है। यूरोप में ऐसे ही अस्तित्व के संकट से आयरिश, सिसिली और यिडिश भाषाएं भी जूझ रही हैं।
हमें याद रखना चाहिए कि भाषाओं की गहन विविधता सांस्कृतिक विविधता को ना सिर्फ सुनिश्चित करती है, बल्कि अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है। अगर आज के दौर में किसी भाषा को पीछे धकेला जा रहा है या किनारे किया जा रहा है तो इसका मतलब यह भी है कि इसके जरिए एक तरह से उस भाषा विशेष के इलाके की संस्कृति का हिस्सा भी गायब हो रहा है। हर संस्कृति में सबकुछ लिखने की क्षमता नहीं होती, उसके कई तत्व श्रुति, स्मृति और चलन के सहारे जिंदा रहते हैं। भाषा के मरने के बाद संस्कृति का यह अलिखा हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी भाषाओं को जिंदा रखें। भाषाओं को जिंदा रखने के लिए स्थानीय स्तर पर कोशिशें भी हो रही हैं। चीन ने अपनी पुरानी मंदारिन को संरक्षित करने के लिए अभियान चला रखा है। नाइजीरिया अपनी भाषाओं को वाचिक रूप में बचाए रखने के लिए रिकॉर्ड करने का सहारा ले रहा है। भारत में भी कई लोग अपनी बोलियों के लिए ऐसी कोशिशें कर रहे हैं। मरती हुई भाषाओं के लिए व्यक्तिगत की बजाय सामूहिक कोशिशें होनी चाहिए।
भाषाएं क्यों जरूरी हैं, इसे हमें अमेरिकी नारी वादी रीटा मे ब्राउन के शब्दों में समझ सकते हैं। रीटा कहती हैं, “भाषा किसी भी संस्कृति का रोडमैप होती है। वह आपको बताती है कि इसे बोलने वाले लोग कहां से आते हैं और कहां जा रहे हैं।”
-उमेश चतुर्वेदी
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं)
अन्य न्यूज़