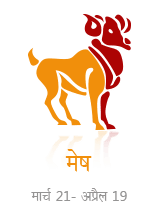गांवों की उपेक्षा कर अनियोजित तरीके से बसाए जा रहे शहर पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा

पर्यावरण एवं प्रकृति को हो रहे नुकसान का मूल कारण अनियोजित शहरीकरण है। बीते दो दशकों के दौरान यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी है। लोगों ने दिल्ली एवं ऐसे ही महानगरों की सीमा से सटे खेतों पर अवैध कालोनियां काट लीं।
कोरोना की उत्तरकालीन व्यवस्थाओं पर चिन्तन करते हुए बढ़ते पर्यावरण एवं प्रकृति विनाश को नियंत्रित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, इसके लिये बढ़ते शहरीकरण को रोकना एवं गांव आधारित जीवनशैली पर बल देना होगा। भले ही शहरीकरण को आर्थिक और सामाजिक वृद्धि का सूचक माना जाता है। लेकिन अनियंत्रित शहरीकरण बड़ी समस्या बन रहा है। भारत में तो शहरीकरण ने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं, आम जनजीवन न केवल स्वास्थ्य बल्कि जीवनमूल्यों की दृष्टि से जटिल होता जा रहा है। आर्थिक विकास भी इसी कारण असंतुलित हो रहा है। ऐसे में जब कोरोना जैसे अभूतपूर्व संकट के दौरान बेतरतीब जीवनशैली से भरे शहर अचानक डराने लगें तब हमारे गांवों ने ही शहरी लोगों को पनाह दी। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी योजनाएं बनाई जाएं जिससे गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को होने वाले पलायन की रफ्तार कुछ थम सके।
इसे भी पढ़ें: कोरोना और पराली से परेशानी क्या कम थी जो आतिशबाजी भी कर दी गयी
पर्यावरण एवं प्रकृति को हो रहे नुकसान का मूल कारण अनियोजित शहरीकरण है। बीते दो दशकों के दौरान यह प्रवृत्ति पूरे देश में बढ़ी है। लोगों ने दिल्ली एवं ऐसे ही महानगरों की सीमा से सटे खेतों पर अवैध कालोनियां काट लीं। इसके बाद जहां कहीं सड़क बनी, उसके आसपास के खेत, जंगल, तालाब को वैध या अवैध तरीके से कंक्रीट के जंगल में बदल दिया गया। देश के अधिकांश उभरते शहर अब सड़कों के दोनों ओर बेतरतीब बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल स्वतन्त्र भारत के विकास के लिए हमने जिन नक्शे कदम पर चलना शुरू किया उसके तहत बड़े-बड़े शहर पूंजी केन्द्रित होते चले गये और रोजगार के स्रोत भी ये शहर ही बने। शहरों में सतत एवं तीव्र विकास और धन का केन्द्रीकरण होने की वजह से इनका बेतरतीब विकास स्वाभाविक रूप से इस प्रकार हुआ कि यह राजनीतिक दलों के अस्तित्व और प्रभाव से जुड़ता चला गया, लेकिन पर्यावरण एवं प्रकृति से कटता गया। इसी कारण गांव आधारित अर्थ-व्यवस्थाएं लडखड़ाने लगी हैं।
बढ़ते शहरीकरण के बावजूद एक बड़ा सच यह भी है कि आज भी देश में सत्तर फीसद आबादी गांवों में बसती है। यानी अगर शहरीकरण को विकास का पैमाना मान भी लिया जाए तो हम दुनिया के ज्यादातर देशों से अभी बहुत पीछे हैं। बहरहाल, कितने भी पीछे हों, लेकिन जितना और जैसा समस्याबहुल शहरीकरण हो रहा है उसने गंभीर सोच-विचार के लिए हमें मजबूर कर दिया है। खासकर तब, जब शहरीकरण की मौजूदा चाहत के चलते अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक देश की शहरी आबादी गांवों की आबादी से ज्यादा हो जाएगी।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में कहा कि उम्मीद के मुताबिक भारत की 40 प्रतिशत आबादी 2030 तक शहरी क्षेत्रों में रहेगी और हमें इसके लिए छह से आठ सौ मिलियन वर्ग मीटर का अर्बन स्पेस बनाना होगा। पुरी के अनुसार 100 स्मार्ट सिटी में 1,66,000 करोड़ रुपये की लगभग 4,700 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो प्रस्तावित कुल परियोजनाओं का लगभग 81 प्रतिशत है। सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है बढ़ते शहरीकरण को नियोजित करने की। शहरों में अधिक आबादी रहने का मतलब है कि उनका आधारभूत ढांचा संवारने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए ताकि वे बढ़ी हुई आबादी का बोझ सहने में समर्थ रहें और साथ ही रहने लायक भी बने रहें। लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग है। हमारे जिन भी नीति नियंताओं और विभागों पर भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शहरी ढांचे का निर्माण करने की जिम्मेदारी होती है, वे शहरों के नियोजन के नाम पर कामचलाऊ ढंग से काम करते हैं। नया शहरीकरण अनियोजित और मनमाना होता है, जहां पर सिर्फ कंक्रीट के जंगल होते हैं तो पुराने इलाके में पूरा ढांचा ही जर्जर और गंदगी से भरा होता है। इसका नतीजा यह होता है कि हमारे देश में शहरों की परिभाषा तरह-तरह के प्रदूषणों, गंदगी, वायु दूषित होने, अतिक्रमण, अपराध, ट्रैफिक जाम, जलभराव, झुग्गी बस्तियों, अनियंत्रित निर्माण और कूड़े के पहाड़ के बगैर पूरी ही नहीं होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पहले ही कार्यकाल में स्मार्ट सिटी की अवधारणा लेकर आए थे। लेकिन यह योजना भी भ्रष्टाचार, पैसे की तंगी और अनियमितता की भेंट चढ़ गई। यह योजना केंद्र सरकार और राज्यों के बीच टकराव का कारण भी बन गई। इसके साथ ही एक समस्या यह भी है कि सिर्फ फ्लाईओवर, मेट्रो आदि का निर्माण करके हमारे नीति नियंता शहरीकरण के नाम पर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं लेकिन क्या इससे शहरों में रहने लायक स्थिति बन जाती है ? क्या बढ़ता शहरीकरण पर्यावरण एवं प्रकृति के लिये गंभीर खतरा नहीं बन रहा है ?
इसे भी पढ़ें: साक्षात्कारः पर्यावरणविद् सुनीता नारायण ने बताये प्रदूषण से निजात के उपाय
भारत की अर्थ-व्यवस्था आज भी गांव, कृषि, पशुपालन आधारित है। असली भारत आज भी गांवों में ही बसता है जिसमें देश की करीब 70 फीसद आबादी रहती है। दरअसल वास्तविकता यह है कि हमने आजादी के बाद से लेकर अब तक गांवों एवं गांव आधारित स्वस्थ, उन्नत एवं आत्मनिर्भर जीवन को नकारा है। गांवों की उन्नति एवं उन्हें बेहतर बनाने की बजाए हमने उनकी उपेक्षा की है, जिससे वहां से पलायन बढ़ा है। हमारी सरकारें शहरीकरण के नाम पर हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के लिए तैयार हैं लेकिन गांवों में मूलभूत सुविधाओं के नाम पर भी पैसा देने से उन्हें तकलीफ होने लगती है। गांवों को लेकर सरकार की नीतियां विसंगतिपूर्ण रही हैं। खेती को घाटे का सौदा बता दिया गया और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को निराश करने वाली व्यवस्था में बदल दिया गया। खेती को मुनाफे का सौदा बनाने और गांवों की अर्थव्यवस्था में निवेश करने की बजाय पूरा ध्यान गांवों की जनसंख्या को शहरों में खींच लेने पर रहा।
गांवों के प्रति उपेक्षा से जुड़ी हकीकत यह है कि बड़ी आबादी वहां रहने के बावजूद पेयजल की सप्लाई नहीं है, चिकित्सा-सुविधाएं नगण्य हैं। प्रति व्यक्ति बिजली की खपत देखी जाए तो गांव काफी पीछे हैं लेकिन इसके बावजूद बिजली कटौती की सबसे ज्यादा मार ग्रामीण इलाकों पर ही पड़ती है। गांवों में शिक्षा का ढांचा आज भी जर्जर है। बीते सात दशकों में रोजगार सृजन को लेकर गांवों की अनदेखी की गई है। गांवों की परिवहन समस्याओं के प्रति भी हमारी सरकारें उदासीन रही हैं।
हमारे देश में संस्कृति, मानवता और जीवन का विकास नदियों के किनारे एवं गांवों में ही हुआ है। सदियों से नदियों की अविरल धारा और उसके तट पर मानव जीवन फलता-फूलता रहा है। बीते कुछ दशकों में विकास की ऐसी धारा बही कि नदी की धारा आबादी के बीच आ गई और आबादी की धारा को जहां जगह मिली वह बस गई। और यही कारण कि हर साल कस्बे नगर बन रहे हैं और नगर महानगर। बेहतर रोजगार, आधुनिक जनसुविधाएं और उज्ज्वल भविष्य की लालसा में अपने पुश्तैनी घर-बार छोड़कर शहर की चकाचौंध की ओर पलायन करने की बढ़ती प्रवृत्ति का परिणाम है कि देश में एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या लगभग 350 हो गई है जबकि 1971 में ऐसे शहर मात्र 151 थे। यही हाल दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का है।
महानगर केवल पर्यावरण प्रदूषण ही नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रदूषण की भी गंभीर समस्या उपजा रहे हैं। लोग अपनों से, मानवीय संवेदनाओं से, अपनी लोक परंपराओं व मान्यताओं से कट रहे हैं। जिसके कारण परम्परा एवं संस्कृति में व्याप्त पर्यावरण एवं प्रकृति संरक्षण के जीवन सूत्रों से हम दूर होते जा रहे हैं, ऐसे कारणों का लगातार बढ़ना, नगरों- महानगरों का बढ़ना, जनसंख्या बहुल क्षेत्रों का सुरसा सतत विस्तार पाना और उसकी चपेट में प्रकृति और उसकी नैसर्गिकता का आना गंभीर स्थितियां हैं। इंसान की क्षमता, जरूरत और योग्यता के अनुरूप उसे अपने मूल स्थान पर यानी गांवों में अपने सामाजिक सरोकारों के साथ जीवन-यापन का हक मिले, विकास का अवसर मिले। यदि विकास के प्रतिमान ऐसे होंगे तो शहर की ओर लोगों का पलायन रूकेगा। इससे हमारी धरती को कुछ राहत अवश्य मिलेगी। प्रकृति एवं पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरों में भी तभी कमी आयेगी।
-ललित गर्ग
अन्य न्यूज़