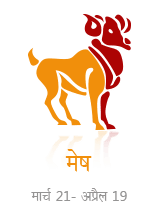चौथे स्तंभ की अहमियत और मीडिया का बदलता स्वरूप

बड़े या छोटे ''प्रिंट मीडिया'' के पास पाठक ही नहीं दिखते हैं। इंटरनेट क्षेत्र में आयी क्रांति और उसके बाद मोबाइल क्रांति ने तो इस क्षेत्र के सभी पाठकों को झटके से छीन लिया है।
लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ 'मीडिया' की बातें और उसकी धुंधली होती कार्यशैली पर चर्चाएं अक्सर होती ही रहती हैं। कोई इसके लिए बदलते समय को दोषी ठहराता है तो कोई अर्थ की प्रधानता को। मुश्किल यह है कि इन चर्चाओं में किसी प्रकार का लब्बो लुआब निकल कर सामने नहीं आता, जिससे इन समस्याओं का निदान हो सके। अख़बार मालिक और तमाम पत्रकार बंधु इस क्षेत्र में कमाई के स्रोत निरन्तर कम होने से खुद ही परेशान रहते हैं तो दूसरी ओर पीत पत्रकारिता एवं ब्लैकमेलिंग जैसे शब्दों ने इस पेशे को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कई मित्रों से मुलाकात में इन विषयों पर चर्चा होती ही रहती है, जिसमें डीएवीपी में विज्ञापन से लेकर, बदलती तकनीक का प्रयोग तक शामिल रहता है, जिससे लोकतंत्र के इस चौथे स्तम्भ की वर्तमान में जद्दोजहद सामने आती है। इससे जुड़ी समस्याओं, आर्थिक पहलु की बातें एवं समाधान की कुछ बातें साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ-
वर्तमान मीडिया का अर्थशास्त्र: हमारे सामने कई बार यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि कई अखबार और पत्रिकाएं होने के बावजूद, उनमें से कितनी बनती और छपती हैं? यह एक विकराल सच है कि मात्र फ़ाइल कॉपी का जुगाड़ करके बहुत से अख़बार, पत्र-पत्रिकाएं 'डीएवीपी' से विज्ञापन उठा लेती हैं। कई अख़बारों और पत्रिकाओं की हालत को तो हम आप सहित अनेक लोग जानते होंगे कि किस प्रकार 10% से लेकर 20 और 25% तक के कमीशन आज मोदीराज में भी डीएवीपी के 99 फीसदी अधिकारियों के पास प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में पहुँचते हैं और उसके बदले अखबार न छापने और सर्कुलेशन का लम्बा झोल करने का वह लाइसेंस दे देते हैं। कई लोग तो 'डीएवीपी' से ऐसा काम करके ही रोटी-रोजी चला लेते हैं किन्तु, जिनके अंदर कहीं पत्रकारिता बची हुई है, वह आखिर क्या करें? अब तो 'लाइजनिंग, दलाली और ब्लैकमेलिंग' जैसे शब्द, दुर्भाग्य से इस पेशे की पहचान बन चुके हैं! यह चलन आम हो गया है और फिर इसमें क्या किया जा सकता है, इस बात का किसी के पास शायद ही जवाब हो! कई लोग वेबसाइट, ब्लॉग इत्यादि को देखकर थोड़ी उम्मीद जगाते हैं कि 'शायद पत्रकारिता और लेखन' को कोई राह मिल जाए! किन्तु इस राह में भी कम दुश्वारियां कहां हैं? बढ़ता खर्च, टेक्नोलॉजी का झोल और यूनिक कंटेंट की कमी सबसे बड़ी मुसीबत के तौर पर सामने आ खड़ी होती है।
मीडिया क्षेत्र में गिरावट का कारण: मिशन का अभाव, कॉर्पोरेट घरानों का कब्ज़ा, प्रिंट मीडिया की गिरती अहमियत और इन सबसे बढ़कर छोटे-मझोले अख़बारों के साथ पत्रकारों की कमाई के स्रोत सूख जाना, जैसे विषय इस क्षेत्र के सुधीजनों को परेशान किये हुए हैं। आज आखिर कौन अपने बेटों को इस क्षेत्र में लाना चाहता है? थोड़ा व्यापक रूप से गौर किया जाए तो इस क्षेत्र में जो कठिनाइयां आयी हैं, उनका बड़ा कारण तकनीक की समझ और उसके प्रयोग को लेकर नज़र आता है। फिर वह चाहे मीडिया के मिशन की बात हो अथवा इसके अर्थशास्त्र को लेकर ही उहापोह क्यों न हो। थोड़ा और स्पष्ट करें तो बड़े या छोटे 'प्रिंट मीडिया' के पास पाठक ही नहीं दिखते हैं। इंटरनेट क्षेत्र में आयी क्रांति और उसके बाद मोबाइल क्रांति ने तो इस क्षेत्र के सभी पाठकों को झटके से छीन लिया है, जिसकी भनक छोटे तो छोड़िए, बड़े अख़बार समूहों तक को नहीं लगी, जिसका नतीजा उन्हें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भुगतना ही पड़ा। हाँ, टाइम्स इंटरनेट (टाइम्स समूह) जैसे कुछ समूहों ने वक्त की नज़ाकत भांपते हुए जरूर इस क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत की।
अंग्रेजी मीडिया इस तकनीकी परिवर्तन को भांपने में काफी आगे रहा तो हिंदी मीडिया का 80 फीसदी हिस्सा इस परिवर्तन को समझने में चूक सा-गया। हालाँकि, भास्कर, जागरण, प्रभासाक्षी जैसे कुछ छोटे-बड़े नाम इसमें जरूर लगे रहे। दूसरे भी कई नामों ने इसमें हाथ आजमाने की कोशिश जरूर की, परन्तु उनका संघर्षकाल तकनीकी जानकारियों की गम्भीरता के अभाव में लम्बा खिंच गया। इससे भी बड़ी बात यह हुई कि प्रिंट मीडिया का क्षेत्र काफी समय से इंटरनेट का पिछलग्गू-सा बन कर रह गया है। आप अख़बार, पत्रिका कुछ भी उठाकर देख लीजिए और उसके दो चार लेखों या ख़बरों का एक पैरा गूगल में डाल कर देखिये तो आपको अहसास हो जायेगा कि उसे गूगल के माध्यम से किसी वेबसाइट या ब्लॉग से उठाकर छापा गया है। ऐसी स्थिति में पाठकों का छिटकना अस्वाभाविक कहाँ है? हाँ, कुछ पुराने लोग जो इंटरनेट इत्यादि से साम्य बिठा पाने में मुश्किल महसूस करते हैं वह जरूर अख़बार, पत्रिकाओं के पाठक बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त, जिन लोगों को अपने लेख, फोटो देखने की आदत होती है, वह भी अख़बार का खुद से सम्बंधित हिस्सा देख लेते हैं।
कंटेंट की अहमियत: अपनी वेबसाइट के पिछले कई साल के अनुभव साझा करूँ तो कई अख़बार और पत्रिका के लोगों ने मुझसे वेबसाइट बनवाई तो कई ने मुझसे इसे संचालित करने को भी कहा, किन्तु महीनों बाद भी जब नतीजा 'ढाक के तीन पात' ही रहा तब उनका मन इससे उचट गया, जो स्वाभाविक ही था। कई लोगों ने मुझसे यह कहा कि अमुक कीवर्ड पर मेरी वेबसाइट गूगल के टॉप पर चाहिए, आप ला दीजिये। ऐसे लोगों से जब मैंने नित नए कंटेंट की मांग शुरू की, मसलन एक्सक्लूसिव न्यूज, आर्टिकल्स तब पत्रकारों और सम्बंधित अधिकांश सम्पादकों का अनोखा जवाब था कि दूसरी जगह से उठाकर डाल दीजिये वेबसाइट पर, गूगल पर सब मिलता है। मुझे भारी आश्चर्य हुआ क्योंकि इस पेशे की मैं इज्जत करता था अब तक और वह सिर्फ इसलिए कि इस क्षेत्र के लोग विचारवान होते हैं, लिखकर दूसरों तक अपने सटीक विचार पहुंचाते हैं।
जहाँ तक गूगल और इंटरनेट पर भी अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की पॉपुलैरिटी की बात है तो वहां भी 90 फीसदी से ज्यादा अहमियत 'यूनिक कंटेंट' की ही है। बाकी 10 फीसदी में मेटा, कीवर्ड, बैकलिंक इत्यादि कुछ कार्य हैं, किन्तु अगर आपका कंटेंट दमदार और सबसे अलग नहीं है तो आप अपनी वेबसाइट पर खूब मसाला डालिए, किन्तु कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। यह एक ऐसा तथ्य है, जिससे संपादक और पत्रकार जान बूझकर अपनी आँखें चुराते हैं। यह बात दावे से कही जा सकती है कि अगर एक साल तक, प्रतिदिन हज़ार शब्दों का 1 यूनिक लेख अपनी वेबसाइट या ब्लॉग पर आप डालते हैं और 10 फीसदी कीवर्ड, टैग, सबमिशन इत्यादि गतिविधियाँ (आसान है यूट्यूब से सीखना, समझना) करते हैं तो कोई कारण नहीं कि 365 लेख आपकी पहचान को स्थापित कर दें। इतना ही नहीं, पत्रकार और संपादक महाशयों को इस क्षेत्र से इतनी बड़ी ऑपर्चुनिटी दिखाई देगी कि वह 'डीएवीपी' की दलाली की बजाय शान से यूनिक विजिट के दम पर विज्ञापन लेने की सार्थक कोशिश कर सकते हैं। वैसे भी सुनने में आया है कि डीएवीपी (डायरेक्टोरेट ऑफ़ विजुअल एडवर्टिजमेंट एंड पब्लिसिटी) ऑनलाइन मीडिया के लिए एक अलग सेक्शन बनाने जा रही है। यह प्रावधान अभी भी है, किन्तु इसमें अभी तक के नियम अव्यवहारिक बताये जा रहे हैं। गूगल के एडसेंस से लेकर, दर्जनों अफिलिएट प्रोग्राम का रास्ता है, जो सीधे आपके पाठकों से जुड़ा हुआ है यदि यह भी रास्ता आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता है तो फ्रीलांसर.कॉम, अपवर्क.कॉम, कन्टेन्टमार्ट.कॉम जैसी सैंकड़ों वेबसाइट हैं जो आपकी क्षमता का उपयोग करने के लिए पूरी विश्वसनीयता से कार्य कर रही हैं।
तकनीकी पक्ष: यह बात भी सच है कि जानकारी के अभाव में कई पत्रकार या संपादक वेबसाइट शुरू करते तो हैं, किन्तु कुछ ही समय बाद उनको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि वह ठग लिए गए हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं हालाँकि, इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा विषय नहीं है, किन्तु इसके लिए ध्यान जरूर देना होगा और क्रमिक रूप से सफर को लगातार जारी रखना होगा। अगर कोई पत्रकार मित्र हैं तो शुरू में उनके लिए ब्लॉग बनाना ही फायदेमंद है और अगर इसे वह छः महीनों तक लगातार चला पाने की इच्छाशक्ति दिखा पाते हैं तो फिर ब्लॉग को कस्टमाइज करा लेने से इसकी ख़ूबसूरती बढ़ जाएगी। इसे यूट्यूब पर खुद भी सीखा जा सकता है अथवा किसी योग्य की मदद लेकर शुरूआती रूप में कुछ हजार में कस्टमाइज कराया जा सकता है। फिर धीरे-धीरे आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ऐडसेंस इत्यादि में कमाई के स्रोत ढूंढ सकते हैं तो पाठकों की संख्या और उनकी प्रतिक्रिया भी काफी मायने रखेगी। इसके लिए आप ब्लॉगर.कॉम, टुंबलर.कॉम, वर्डप्रेस.कॉम जैसे पॉपुलर और कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आप इन्हीं ब्लॉग अड्रेस को अपने डोमेन का नाम दे सकते हैं।
अख़बार या पत्रिकाओं में अपेक्षाकृत ज्यादा अपडेट होती है तो उसके लिए कई सेक्शन बनाने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त, आपको ईपेपर, ईमैगजीन भी अपलोड करनी पड़ती है। इसके लिए आपको बाकायदा वेबसाइट बनाना ही ठीक रहेगा, किन्तु कस्टमाइज वेबसाइट से हज़ार गुना बेहतर और सुविधाजनक रहेगा ओपन सोर्स 'सीएमएस' का चुनाव, जैसे वर्डप्रेस, जुमला, द्रुपल इत्यादि। इनमें भी वर्डप्रेस का चुनाव आसान है। जाहिर है, शुरुआत में आपको बाजार से मदद लेनी पड़ेगी, किन्तु कोई आपको धोखा नहीं दे सके इसके लिए आप खुद भी चुने हुए प्लेटफॉर्म की जानकारी लेने का समय निकालें। फ़ाइल और डेटाबेस का बैकअप लेते रहें। बाकी, यूनिक कंटेंट आप डालते हैं और सोशल मीडिया, ईमेलर इत्यादि से प्रचार शुरू करते हैं तो निश्चित ही आपकी वेबसाइट लाभ अर्जित करेगी।
अन्य न्यूज़