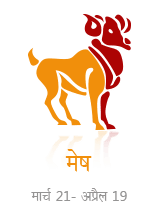गंगा की निर्मलता के लिए उसका अविरल बहना जरूरी

यदि गंगा अविरल बहेगी, तो वह स्वाभाविक रूप से निर्मल होगी ही। इस दौरान उसमें यदि धूल या पत्ते जैसी कुछ गंदगी मिलेगी भी, तो धूप और बहती हवा उससे समाप्त कर देगी और पानी फिर निर्मल हो जाएगा।
गंगा की चर्चा होते ही उसकी अविरलता और निर्मलता की बात होने लगती है। ‘बहता पानी निर्मला’ वाली कहावत के अनुसार यदि गंगा अविरल बहेगी, तो वह स्वाभाविक रूप से निर्मल होगी ही। इस दौरान उसमें यदि धूल या पत्ते जैसी कुछ गंदगी मिलेगी भी, तो धूप और बहती हवा उससे समाप्त कर देगी और पानी फिर निर्मल हो जाएगा। इसलिए न केवल गंगा, बल्कि सभी नदियों की निर्मलता के लिए उनका अविरल बहना जरूरी है।
लेकिन इसके साथ ही एक दूसरा प्रश्न भी उभरता है कि बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण से पानी की जरूरत में जो वृद्धि हुई है, वह कैसे पूरी होगी ? जनसंख्या वृद्धि से अन्न की मांग बढ़ी है। उद्योग धन्धों एवं शहरीकरण के विस्तार से खेती की जमीन लगातार घट रही है। अतः कृषि वैज्ञानिकों ने जल्दी उगने वाले खाद्य पदार्थ तथा साल में दो की बजाय तीन या चार फसलें उगाने की विधियां खोजीं हैं। ऐसे में अधिक पानी खर्च होना ही है। तो यह पानी कहां से आएगा ? इसलिए नदियों पर बांध और धरती की कोख से पानी खींचने वाले यंत्र बने। अतः हर समय पानी मिलने लगा।
लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। कुएं और हाथनलों के जमाने में हमें पानी के लिए कुछ श्रम करना पड़ता था; पर अब तो बिजली का बटन दबाते ही पानी हाजिर हो जाता है। अतः जो काम पहले 20 लीटर में हो जाता था, अब वह 200 लीटर में भी पूरा नहीं होता। फिर वोटों की फसल काटने हेतु ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली जैसे उपायों ने धरती की कोख ही सुखा दी है। पहले 50 फुट पर पीने का साफ पानी मिल जाता था; पर अब 250 फुट से खींचने के बाद भी उसे फिल्टर करना पड़ता है। अर्थात सही हो या गलत, पर हमारी पानी की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। ऐसे में एकमात्र उपाय बांध ही है; और बांध बनते ही कोई भी नदी अविरल नहीं रहती।
दूसरी बात निर्मलता की है। इसमें सबसे अधिक बाधक नदियों में गिरने वाले गंदे नाले, सीवर और उद्योगों से निकला दूषित पानी है। इन्हें रोकने के लिए जहां एक ओर राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए, वहां हमारी मानसिकता भी इसमें सहयोगी हो सकती है। कुछ वर्ष पूर्व एक सर्वेक्षण दल ने गंगोत्री से गंगासागर और फिर गंगोत्री तक की यात्रा की। यात्रा के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें गंगा के किनारे कोई नगर ऐसा नहीं मिला, जिसकी गंदगी गंगा में न जाती हो। दूसरी ओर ऐसा कोई गांव भी नहीं मिला, जिसकी गंदगी गंगा में जाती हो। अर्थात गंगा को गंदा करने का पाप मुख्यतः नगरवासी ही कर रहे हैं।
चमड़ा उद्योगों का एक प्रमुख केन्द्र कानपुर है। उनका रासायनिक अपशिष्ट गंगा में गिरता है। हर सरकार उन्हें वहां से हटा कर कहीं और ले जाने की बात कहती है; पर हटा नहीं पाती। क्योंकि उन उद्योगों से बड़ी संख्या में मुसलमान जुड़े हैं। उ.प्र. की राजनीति में मुसलमानों को नाराज करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। यही स्थिति गंगा के किनारे स्थित अन्य उद्योगों की भी है। लोग बार-बार लंदन की टेम्स नदी का उदाहरण देते हैं, जिसे 30 साल में स्वच्छ कर दिया गया; पर यह भी याद रहे कि वहां जाति या मजहब के नाम पर राजनीति नहीं होती। जबकि भारत में राजनीति का प्रमुख आधार ही ये दोनों हैं। अतः औद्योगिक गंदगी से गंगा को बचाने के लिए प्रबल राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए।
जहां तक गंगा में मानव मल (सीवर) गिरने की बात है, तो नगरों में विकास के नाम पर जिस व्यवस्था को केन्द्रित कर दिया गया, उसे फिर से विकेन्द्रित करना होगा। मेरा गांव गंग नहर के किनारे ही बसा है। लगभग 45 साल पहले हमारे घर में फ्लश वाले शौचालय बने। उन दिनों वहां सरकारी सीवर लाइन नहीं थी। अतः मकान में एक ओर सैप्टिक टैंक बनाया गया था। मिस्त्री ने उसमें कुछ गोबर आदि डालकर कहा था कि इसमें जो कीड़े पैदा होंगे, वे मानव मल को लगातार खाते रहेंगे। इस प्रकार यह 30-35 साल तक ठीक से काम करेगा। उसके बाद इसे साफ कराना होगा। उसने यह भी बताया था कि इसमें साबुन का पानी नहीं डालना। अन्यथा ये कीड़े मर जाएंगे। ऐसे सैप्टिक टैंक उस मोहल्ले के सभी घरों में बने थे।
पर कुछ साल बाद गांव में सरकारी सीवर लाइन पड़ गयी, तो निजी सैप्टिक टैंक समाप्त हो गये। पहले लोग शौचालय में साबुन का पानी डालने से यह सोचकर बचते थे कि इससे उनका निजी सैप्टिक टैंक खराब हो जाएगा; पर अब इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। और इसका दुष्परिणाम सबके सामने है ही। इसलिए सारे गांव या नगर के सीवर को एक साथ जोड़ने की बजाय उसे घर, मोहल्ले या कालोनी के स्तर पर ही पुनर्चक्रित कर निबटाना होगा। जब यह गंदगी गंगा में पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर उसके प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण ही समाप्त हो जाएगा।
आजकल हरिद्वार और काशी की देखादेखी गंगातट पर बसे अनेक नगरों में शाम को गंगा आरती होने लगी है। केवल गंगा ही नहीं, तो अन्य नदियों को भी पूजने का अंधा चलन हो गया है। पूजा के लिए पर्यटक और स्थानीय लोगों की भीड़ वहां एकत्र हो जाती है। इस मेले से नदी का तट और आसपास की सड़कें और अधिक गंदी हो जाती हैं। लोग नदी में अपने घर की बासी पूजा सामग्री भी डाल देते हैं। यह नदी की पूजा है या उस पर अत्याचार ? वस्तुतः नदी की पूजा का अर्थ केवल घंटा बजाना नहीं, वरन उसकी सफाई है।
जो गांव या नगर नदी या नहरों के तट पर बसे हैं, वहां स्नान घाट भीषण गंदे रहते हैं; पर इसके लिए सरकारों को कोसने की बजाय जनता को भी जागरूक और सक्रिय होना होगा। यहां मैं पुरानी टिहरी का उदाहरण दूंगा। वहां भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम होता था। वह ऐतिहासिक नगर अब टिहरी बांध में समा गया है।
टिहरी में बड़ी संख्या में लोग प्रातःकालीन कामों के लिए नदी के किनारे ही जाते थे। इससे वहां गंदगी हो जाती थी। ऐसे में कई बुजुर्गों ने मिलकर एक योजना बनायी। वे सामूहिक रूप से अति प्रातः ही नदी के तट पर पहुंच जाते थे। उनके हाथ में डंडा होता था तथा गले में सीटी। जो कोई नदी के पास बैठने लगता था, वे उसे डंडा दिखाकर दूर जाने को कहते थे। यदि कोई नहीं मानता था, तो वे सीटी बजाकर अपने सब साथियों को बुला लेते थे। इतने लोगों को देखकर उसे वहां से भागना ही पड़ता था। उनके प्रयास से फिर लोग स्वयं ही लोटे या बोतल में पानी लेकर तट से दूर बैठने लगे। इस प्रकार तट साफ रहने लगा।
सच तो यह है कि बुजुर्गों का यह प्रयास ही नदी की वास्तविक पूजा है। किसी का यह कथन ठीक ही है कि गंगा को साफ करने की जरूरत नहीं है। उसमें तो स्वयं को साफ करते रहने का अद्भुत गुण विद्यमान है। आवश्यकता बस इतनी है कि हम उसे गंदा न करें और उसे निर्बाध बहने दें।
गंगा के साथ एक विडम्बना और भी है। राजीव गांधी के समय से इसकी स्वच्छता के सरकारी प्रयास हो रहे हैं। अरबों-खरबों रु. इसमें बह चुका है; पर गंगा क्रमशः और अधिक गंदी ही हुई है। इसका कारण है सुस्पष्ट योजना का अभाव। हर सरकार और मंत्री के पास अपने विशेषज्ञ और ठेकेदार होते हैं, जो उनके साथ सक्रिय हो जाते हैं; पर सरकार और मंत्री बदलते रहते हैं। अतः बार-बार योजनाएं भी बदलती हैं और परिणाम वही ढाक के तीन पात।
इसलिए गंगा को सुधारना है, तो राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक जागरूकता, विशेषज्ञों द्वारा निर्मित समयबद्ध योजना, कठोर कानून और उनका पालन, धर्म, विज्ञान और वर्तमान जनसंख्या की जरूरतों में व्यावहारिक समन्वय जैसे मुद्दों पर एक साथ काम करना होगा, तब जाकर जगत कल्याणी मां गंगा स्नान और ध्यान, वंदन और आचमन के योग्य बन सकेगी।
- विजय कुमार
अन्य न्यूज़