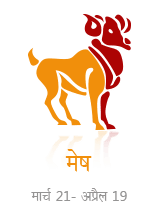कई ऐसे मुद्दे जिनसे पाक को दबाव में लाना संभव है

तात्कालिक रूप में सिंधु जल संधि और दोनों देशों के मध्य परस्पर व्यापार को बढ़ाने के तहत पाकिस्तान को दिया गया ''मोस्ट फेवर्ड नेशन'' का दर्जा ऐसे बिन्दु हैं जिनकी भारत को तत्काल समीक्षा करनी चाहिए।
पाकिस्तान को विश्व समुदाय में अलग-थलग करने की भारतीय कूटनीतिक कवायद के अतिरिक्त भारत को उन मुद्दों पर पुनः ध्यान से देखने की ज़रूरत है जहां उसने स्वयं ही पाकिस्तान को अनुचित लाभ पहुंचाया हुआ है। तात्कालिक रूप में सिंधु जल संधि और दोनों देशों के मध्य परस्पर व्यापार को बढ़ाने के तहत पाकिस्तान को दिया गया 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा ऐसे बिन्दु हैं जिनकी भारत को तत्काल समीक्षा करनी चाहिए। आइए इन पर एक सरसरी निगाह डालते हैं:
पाक से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' का दर्जा वापस लेना:
सिंधु जल संधि की समीक्षा के ठीक एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे की समीक्षा के लिए भी बैठक बुलाई। हालांकि इस विषय पर अभी कोई आधिकारिक बयान भारत सरकार की तरफ से नहीं आया है किन्तु विशेषज्ञों का कयास है कि यह कार्रवाई उन्हीं कोशिशों का हिस्सा है, जिसके तहत उड़ी हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान पर दबाव बना रही है। यहाँ यह उल्लेख आवश्यक है कि भारत की ओर से पाकिस्तान को दिया गया यह दर्जा एक तरफा है। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा कोई दर्जा नहीं दिया है। भारत ने पाकिस्तान को नब्बे के दशक (1996) में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। पाकिस्तान ने 2012 में भारत को एमएफएन यानी विशेष तरजीह देश का दर्जा देने का ऐलान किया था, लेकिन पाकिस्तान ने वादा नहीं निभाया था।
सिंधु जल संधि के प्रावधानों का भारत के पक्ष में उपयोग:
सिंधु जल संधि दो देशों के बीच जल विवाद पर एक सफल अंतरराष्ट्रीय उदाहरण है जिस पर भारत-पाकिस्तान युद्धों का भी प्रभाव नहीं पड़ा। 19 सितंबर 1960 में, आज से 56 वर्ष पूर्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तानी सैनिक शासक राष्ट्रपति अयूब खान ने भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जल की कमी से उपजने वाले विवादों के विशेषज्ञों के अनुसार भारत वियना समझौते के लॉ ऑफ़ ट्रीटीज़ की धारा 62 के अंतर्गत इस आधार पर सिंधु जल संधि से पीछे हट सकता है कि पाकिस्तान आतंकी गुटों का इस्तेमाल उसके खिलाफ़ कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मानना है कि अगर दो राष्ट्रों के बीच मूलभूत स्थितियों में परिवर्तन हो तो किसी भी संधि को रद्द किया जा सकता है। सिंधु नदी का क्षेत्रफल लगभग 12 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका 47% पाकिस्तान, 39% भारत, 8% चीन, और 6% क्षेत्र अफ़गानिस्तान में आता है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 35 करोड़ की आबादी सिंधु नदी के थाले में रहती है।
प्रमुख बिन्दु:
समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया। सतलज, ब्यास और रावी नदियों को पूर्वी नदी बताया गया जबकि झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदी बताया गया। पूर्वी नदियों का पानी, कुछ अपवादों को छोड़े दें, तो भारत बिना रोकटोक के इस्तेमाल कर सकता है। पश्चिमी नदियों का पानी पाकिस्तान के लिए होगा लेकिन समझौते के भीतर इन नदियों के पानी का कुछ सीमित इस्तेमाल का अधिकार भारत को दिया गया, जैसे बिजली बनाना, कृषि के लिए सीमित पानी इत्यादि। भारत को इसके अंतर्गत इन नदियों के 20% जल के उपयोग की अनुमति है जबकि वर्तमान में वह मात्र 7% जल का ही उपयोग इन कार्यों के लिए कर रहा है। अनुबंध में बैठक, कार्यस्थल के निरीक्षण आदि का प्रावधान है। समझौते के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई। इसमें दोनों देशों के कमिश्नरों के मिलने का प्रस्ताव था। पाकिस्तान ने भारत को कई बार इन मसलों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में घसीटा है हालांकि अधिकांशतः मामलों में उसे सफलता नहीं मिली है।
किशन गंगा पर पाकिस्तानी आपत्ति:
भारत की तीन सौ तीस मेगावाट की किशन गंगा जल विद्युत् परियोजना ने पाकिस्तान की नींद हराम कर रखी है। किशन गंगा परियोजना जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी की एक सहायक नदी किशन गंगा पर स्थित है। नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी) के अनुसार इस परियोजना में सैंतीस मीटर ऊंचे कंक्रीट मुख वाला एक राक-फिल (पत्थरों से भरा हुआ) बाँध और एक भूमिगत विद्युत् गृह का निर्माण प्रस्तावित है। कुल मिला कर 697 मीटर सम्मिलित हेड का उपयोग एक सौ दस मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाली तीन इकाइयों की स्थापना के लिए किया जायेगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद उड़ी-1 और उड़ी-2 जल विद्युत् परियोजनाओं से भी तीन सौ मेगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली उत्पादित की जाएगी।
बगलिहार बांध परियोजना पर पाकिस्तानी अड़ंगा:
भारत द्वारा चिनाब नदी पर बनाए जा रहे बगलिहार बांध के डिजाइन को लेकर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय चला गया था। तटस्थ विशेषज्ञ ने सिंधु जल समझौते के तहत बनाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल पर जोर दिया और इसके लिए सुरक्षा तथा पानी के सर्वोत्तम इस्तेमाल को कारण बताया। उन्होंने कहा कि समझौते के सामान्य नियमों के अनुसार अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और विज्ञान के नियमों को अपनाने की अनुमति है। उन्होंने बगलिहार बांध तथा पन बिजली संयंत्र की अवधारणा तथा डिजाइन के मूल्यांकन के बारे में यह टिप्पणी की थी।
तुल-बुल परियोजना में पाकिस्तानी अड़ंगा:
पाकिस्तान किशनगंगा और बगलिहार परियोजना की ही तरह भारत की तुल-बुल परियोजना को भी रोके रखने में कामयाब हुआ है। इस को वूलर बैराज के नाम से भी जाना जाता है। भारत ने 1985 में भारत प्रशासित कश्मीर के बारामूला ज़िले में झेलम नदी पर इस परियोजना का निर्माण शुरू किया था। जिसके अंतर्गत झेलम को नौवहन के लायक बनाकर इसका उपयोग दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने के लिए किया जाना था। भारत इसे तुलबुल नेवीगेशन प्रोजेक्ट कहता है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि भारत झेलम नदी पर जिस वूलर बैराज का निर्माण कर रहा है उससे वह पाकिस्तान का पानी रोकेगा। पाकिस्तानी सरकार की ओर से आपत्ति और जेहादी गुटों की धमकियों के बाद भारत ने 1987 में इस परियोजना का निर्माण रोक दिया था।
सिंधु जल संधि और पाकिस्तान की जल व्यवस्था:
पाकिस्तान के चारों सूबे पानी के मामले में पंजाब को संदेह की नज़र से देखते हैं। सिन्धु नदी जल संधि की दुहाई देने वाला पाकिस्तान स्वयं अपने यहाँ आज तक पानी का न्यायोचित बंटवारा नहीं कर पाया है। उसके पास उत्तरी पाकिस्तान में मंगला और तरबेला बाँध है। दिअमिर भाषा बांध पर उसके पास पैसे की कमी पड़ रही है।
मंगला बांध:
मंगला, यह बाँध झेलम नदी पर बनाया गया है। इसे पाकिस्तान ने वर्ष 1961 में बनाना शुरू किया था। लगभग छह वर्ष पश्चात् वर्ष 1967 में यह बन कर तैयार हुआ। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मीरपुर जिले में स्थित है और यह विश्व का सोलहवां सबसे बड़ा बाँध है। मुख्य बांध 10300 फीट (3100 मीटर) लम्बा है और 454 फीट (138 मीटर) ऊंचा है। इसके इर्द-गिर्द 97 वर्ग मील (ढाई सौ वर्ग किलोमीटर) तक झेलम नदी का जल पसरा हुआ है। बाँध की वास्तविक जल भंडारण क्षमता 5,880,000 एकड़ फीट है। जो कि अब गाद इत्यादि जमा हो जाने की वजह से घट कर 4,750,000 फीट रह गयी है। यह इसकी कुल क्षमता का लगभग बीस प्रतिशत है। पाकिस्तान ने बांध की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से इसकी ऊँचाई बारह मीटर और बढ़ने का फैसला किया है। इससे इसकी क्षमता में अट्ठारह प्रतिशत की वृद्धि होगी, साथ ही इससे 120 मेगावाट अतिरिक्त बिजली भी पैदा की जा सकेगी। वर्तमान में इस बांध से 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। किन्तु बांध की ऊंचाई बढ़ाने में पाकिस्तान के सामने चालीस हज़ार निवासियों के विस्थापन की मुसीबत है। इस बांध के निर्माण में 280 गाँव डूब गए थे जिसमें 1,10,000 लोग विस्थापित हुए थे पाकिस्तान अभी तक इन विस्थापितों को ही न तो समुचित मुआवजा दे पाया है न ही उनके पुनर्वास को अमली जमा पहना पाया है। उसने यह चालाकी अवश्य की कि इनमें से अधिकांश नागरिकों को वर्क परमिट दे कर ब्रिटेन में धकेल दिया।
तरबेला बांध:
यह उत्तरी पाकिस्तान के हरिपुर जिले में स्थित है जो कि इस्लामाबाद से महज़ पचास किलोमीटर दूर है। यह बांध नदी से 148 मीटर ऊंचा है, जिसके 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिन्धु नदी के जल का भण्डारण होता है। इस बांध से 4200 मेगावाट जल विद्युत् का निर्माण होता है। तरबेला बांध पर कार्य 1968 में शुरू किया गया और इसे 1497 मीलियन अमरीकी डालर की लागत से वर्ष 1974 में पूरा कर लिया गया।
ठंडे बस्ते की परियोजनाएं:
सिन्धु नदी पर ही पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के मियाँवाली में कालाबाघ स्थान पर कालाबाघ बांध बनाने की प्रबल इच्छा परवेज़ मुशर्रफ की थी। यह बांध लगभग 79 मीटर ऊंचा होता और इसकी लम्बाई 3350 मीटर होती। इसकी जल भण्डारण क्षमता 6,100,000 एकड़ फीट होती और पाकिस्तान इस से 3600 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता था। किन्तु अन्य पाकिस्तानी सूबों के विरोध के चलते अब यह परियोजना ठन्डे बस्ते के हवाले कर दी गयी है।
दिअमिर, उत्तरी पाकिस्तान के छह जिलों में से एक है। चीन के द्वारा तैयार काराकोरम हाईवे यहीं से गुज़रता है। पाकिस्तान सिन्धु नदी पर यहीं भाषा क्षेत्र में दो सौ बहत्तर मीटर ऊंचा दिअमिर भाषा बांध बनाने की तैय्यारी कर रहा है। इस बांध की जल भंडारण क्षमता लगभग 8,107,132 एकड़ फीट होगी और इस से 4,500 मेगावाट बिजली उत्पादित की जा सकेगी। चीन 4500 मेगावॉट की इस योजना के लिए अरबों रुपये का कर्ज देगा। सिनिहाइड्रो नाम की कंपनी इस परियोजना के विकास पर काम करना चाहती है। किन्तु चीन भी इस परियोजना पर पूरी धनराशि लगाने से कतरा रहा है। भारत-पाकिस्तान के बीच विवादित स्थल पर स्थित होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान भी इस पर अपनी पूँजी फंसाने से बच रहे हैं।
दायमर भाषा बांध चिलास, सिंधु नदी पर प्रस्तावित है। 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य वाली इस परियोजना पर लगभग 14 बिलियन डालर का व्यय अनुमानित था और इसे 12 वर्षों में तैयार होना था। सरकार ने इसके लिए 17 हज़ार एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है और कुछ आरंभिक काम भी शुरू हुआ है। वर्ष 2025 तक तैयार होने वाली इस परियोजना में भी वित्तीय संकट का खतरा है। बहुमहत्वाकांक्षी स्कार्दू-कातजराह बांध से पाकिस्तान को 15 हज़ार मेगावाट बिजली की उम्मीद थी किन्तु यह परियोजना अभी ठंडे बस्ते में ही पड़ी है। आज से लगभग दस वर्ष पूर्व, पंजाब में सिंधु नदी पर परवेज़ मुशर्रफ के शासनकाल में कालाबाघ बांध बस बना ही चाहता था किन्तु पाकिस्तान के अन्य प्रांत पंजाब में यह बांध नहीं बनने देना चाहते थे। उन्हें भय था कि इससे पंजाब अन्य राज्यों का पानी रोक कर बैठ जाएगा और इस बांध से केवल पंजाब को ही फायदा होता साथ ही सिंधु नदी में सदैव के लिए जल की कमी उत्पन्न हो जाती। यह परियोजना अभी शुरू ही नहीं हो पाई है। पाक अधिकृत कश्मीर के विवादित होने की वजह से कोई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान इन परियोजनाओं में हाथ डालते हुए कतराता है।
सिंधु जल संधि पर भारतीय रुख से गहराएगा संकट:
पाकिस्तान की जनसंख्या में दस प्रतिशत की वृद्धि उसे स्थायी रूप से जल कमी वाले क्षेत्र में बदल देगी। पाकिस्तानी जल समस्या का एक अन्य पहलू यह भी है कि उसके सत्तर प्रतिशत जल स्त्रोत उसकी सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित हैं, जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। राष्ट्रीय संदर्भ में, पाकिस्तान को बराबर बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति में अंतर का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न प्रान्तों को आवंटित किए गए जल स्त्रोत की वजह से वहाँ 10 (एमएएफ) मिलियन एकड़ फुट जल की कमी आई है। पाकिस्तान की तीन उच्च जल प्रबंधन एजेंसियां- योजना आयोग, जल एवं विद्युत मंत्रालय (वाटर एंड पावर डिस्ट्रिब्यूशन एजेंसी-वापदा) और सिंधु नदी प्रणाली अथॉरिटी इस तथ्य को स्वीकारती हैं और उनका यह भी मानना है कि इस कारण से वे प्रान्तों को उनके हिस्से में आवंटित 114 (एमएएफ) पानी के बजाय केवल 100 (एमएएफ) पानी ही दे पा रही हैं। पाकिस्तान में प्राकृतिक वर्षा में भी ख़ासी असमानता है। गरमी और वर्षा के दौरान चार महीनों में उसकी नदियों में 75% पानी रहता है जबकि शेष आठ महीनों में इसका औसत घट कर 25% रह जाता है। इसी दौरान उसकी ज़रूरत क्रमशः 60% और 40% की रहती है। वर्तमान में लगभग 13 (एमएएफ) जल को ही संकट से बचाव के लिए सुरक्षित किया जाता है। इस वर्ष 25 फरवरी को सिंधु नदी प्रणाली अथारिटी ने पाकिस्तानी सरकार से अप्रत्याशित अनुरोध किया कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में देश भर में जारी सारी योजनाओं को पाँच वर्षों केलिए रोक दे और उस धन का उपयोग अगले पाँच वर्षों तक युद्ध स्तर पर केवल बांध बनाने में करे ताकि पाकिस्तान 22 (एमएएफ) जल का संरक्षण कर सके। उसका मानना है कि बिना ऐसा किए पाकिस्तान को बराबर पानी की किल्लत झेलनी पड़ेगी। अथॉरिटी ने यह भी उजागर किया है कि उसके नदी जल संसाधन में पिछले दस वर्षों में 9 (एमएएफ) जल की कमी हुई है, जो कि जल प्रबंधन के असफल होने का ज्वलंत उदाहरण है। पाकिस्तान में प्रान्तों के परस्पर असहयोग और उनमें एक दूसरी के प्रति संदेह के चलते कई बांध और जल विद्युत परियोजनाएं अधर में लटकी हुई हैं।
“कोई सेना या बम इतने बड़े भू-भाग को नष्ट नहीं कर सकता जितना कि भारत द्वारा पाकिस्तान के जल स्रोत को जिसने कि पाकिस्तान को जीवित रखा हुआ है, को बंद कर दिए जाने से संभव है।“ यह संदेश विश्व बैंक के तत्कालीन प्रमुख इयूने ब्लैक ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाक़त अली खान को वर्ष 1951 में दिया था। यह हक़ीक़त है। और भारत ऐसा करके पाकिस्तान को एक मरुस्थल में बदल सकता है। यह आकलन मेरा नहीं बल्कि पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार डॉन के संपादकीय का है। भारत के इस चक्रव्यूह में फंसे पाकिस्तान का आर्तनाद कुछ समय तक अवश्य ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुनाई पड़ेगा।
- सुधेन्दु ओझा
अन्य न्यूज़