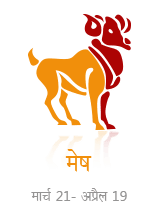बड़ी गड़बड़ है आज की जीवनशैली, तभी बढ़ रहे हैं आत्महत्या के मामले

अभी कुछ दिनों पहले, कथित रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आध्यात्मिक गुरु के खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेने की खबर आई। कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक गुरु ने तनाव के कारण ऐसा किया।
अभी कुछ दिनों पहले, कथित रूप से मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आध्यात्मिक गुरु के खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेने की खबर आई। कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक गुरु ने तनाव के कारण ऐसा किया। अपना तनाव दूर करने के लिए जिन लोगों को आध्यत्मिक गुरु पर भरोसा रहा होगा, उनके लिए ये घटना बेहद चौंकाने वाली है। आजकल आत्महत्या करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अलग-अलग आयु-वर्ग-पृष्ठ्भूमि के लोगों के आत्महत्या कर लेने की ख़बरें अब आम हो चली हैं। आप अख़बार उठा के देख लीजिये, आत्महत्या करने वालों में, स्कूल के छात्र से लेकर, देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग-मेडिकल संस्थानों के अलावा, रसूख वाली नौकरियाँ कर रहे लोग, अभिनेता-अभिनेत्री, पुलिस-सेना, किसान-व्यापारी आदि सभी वर्गों से ताल्लुक रखने वाले शामिल हैं। पिछले एक दशक में शायद ही कोई ऐसा साल रहा हो जिसमें दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षा और उसके बाद आए परीक्षा परिणाम के दौरान कहीं न कहीं किसी छात्र-छात्रा के आत्महत्या कर लेने की खबर न आई हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2018 में आई रिपोर्ट के अनुसार, 2000 से 2015 के बीच आत्महत्या करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है।
2015 में खुदकुशी करने वालों में 18-30 वर्ष के लोगों का प्रतिशत लगभग 33 प्रतिशत रहा है। यदि 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच का आंकड़ा देखें तो इस उम्र समूह में खुदकुशी करने वालों की भागीदारी 66% हो जाती है। 6 प्रतिशत बच्चे, 14 से 18 वर्ष के रहे हैं जिन्होंने 2015 में आत्महत्या की है। आखिर क्यों आत्महत्या करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है ? निश्चित रूप से बढ़ता तनाव और मानसिक स्वास्थ्य का ठीक न होना इसके कारण कहे जायेंगे लेकिन मूल सवाल ये है कि तनाव बढ़ने के क्या कारण हैं ? एक ऐसा देश जो अपने योग-अध्यात्म और आम जन के दार्शानिक तथा संतोषी प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था, आज तनाव से ग्रस्त है। देश में उच्च तनाव से ग्रसित लोगों की संख्या में 2016 से 2017 के बीच चिंताजनक वृद्धि हुई है। उच्च तनाव वाले लोगों के समूह में 116 प्रतिशत की अधिकता दर्ज़ की गई है।
हमारा बदलता सामाजिक ताना-बाना, जिसमें संयुक्त परिवारों का टूटना, गांव से शहरों की ओर पलायन, परिवारों-व्यक्तियों का एकाकीपन और भौतिक संसाधनों की अनावश्यक प्रतिस्पर्धा ने परिवार और व्यक्ति का सुकून छीन लिया है। ज्यादा चीज़ें खरीदने की लालसा और क्रेडिट कार्ड का बिना सोचे-समझे इस्तेमाल से आमदनी से अधिक खर्च करने की आदत, शहरी लोगों में बढ़ी है। बच्चों और वयस्कों में, मोबाइल और इंटरनेट का देर तक मनमाना उपयोग और हिंसक वीडियो गेम्स भी मानसिक असंतुलन को बढ़ा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में, ऑनलाइन और वीडियो गेम्स को मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा बताया है। मोबाइल का देर तक उपयोग करने वाले किशोर वय के समूह में, आक्रमकता बढ़ने का खतरा तो रहता ही है, उनको अनिद्रा और उच्च रक्तचाप होने की प्रबल संभावना बन जाती है।
हमारी रोज़ बढ़ती ज़रूरतों से हमने समाज में प्रतिस्पर्धा का एक ऐसा माहौल बनाया है जिसमें बच्चे से लेकर परिवार तक शामिल है। ब्रांड से ब्रांड की प्रतिस्पर्धा, स्कूल से स्कूल की प्रतिस्पर्धा, छात्रों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने और फिर उस पोजीशन को बनाये रखने की प्रतिस्पर्धा है। युवाओं पर सौ प्रतिशत अंक लाने, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल में प्रवेश लेने और फिर बहुराष्ट्रीय कंपनी में मोटा पैकेज पाने का बाहरी और आंतरिक मानसिक दबाव है। बहुराष्ट्रीय कम्पनी, व्यापार, मैनेजमेंट, फिल्म जगत में अपनी योग्यता और अपनी उपलब्धि को लगातार साबित करने का दबाव रहता है। किसी की लिए भी लगातार उपलब्धि अर्जित करना न तो सहज है न ही स्वाभाविक।
ऐसे में निरंतर दबाव, व्यक्तियों को नई बीमारी की ओर ढकेल देता है। अस्पताल और महँगी दवाओं ने लोगों को इलाज के लिए क़र्ज़ लेने, ज़मीन-जायदाद बेचने और अपने ज़रूरी खर्चों में कटौती के लिए बाध्य किया है। आखिर अपने मानसिक-शारीरिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर के हम कौन सी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं ? बधाई देनी होगी अभिनेत्री दीपिका पादुकोणे को, जिन्होंने कुछ साल पहले सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार किया किया कि वह मानसिक तनाव से गुज़र रही थीं। आत्महत्या करने का विचार आना, एकाकीपन, अनिद्रा, अनावश्यक क्रोध और चिड़चिड़ापन मानसिक तनाव के स्वाभाविक लक्षण हो सकते हैं। मानसिक असंतुलन को स्वीकार करना और मानसिक रोग विशेषज्ञों से परामर्श लेने में कोई सामाजिक छवि बाधक नहीं होनी चाहिए। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की ज़रूरत होती है वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी परामर्श की ज़रूरत पड़ सकती है। बढ़ती आत्महत्या की चिंताओं के बावज़ूद, अभी हमारे देश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बहुत कम है। हालाँकि भारत में मानसिक स्वास्थ्य नीति बनी है लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के प्रोफेशनल्स और पैरा प्रोफेशनल्स की अत्यंत कमी है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं को इस मुद्दे पर जागरूकता के साथ, प्रोफेशनल्स को भी तैयार करने पर विचार करना चाहिए।
लोग अपने स्तर पर भी बदलाव कर सकते हैं। कुछ जागरूक लोग अब अपनी जीवन शैली बदल रहे हैं, तनाव वाली नौकरी छोड़ कर, छोटे शहरों की तरफ सरल जीवन की खोज में जा रहे हैं। अपने खर्चे कम कर रहे हैं और एक कम पेचीदा जीवन जीने की कोशिश में लगे हैं। कुछ लोग 40-45 साल की उम्र में अपने रिटायरमेंट की योजना बना रहे हैं। उसके लिए बचत कर रहे हैं ताकि अपने शौक का भी कुछ कर सकें। कुछ लोग नौकरी से अपनी बुनियादी ज़रूरतों के इंतज़ाम के बाद, सामाजिक कार्य कर रहे हैं क्योंकि हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियों के साथ अगर हमारा सामाजिक योगदान कुछ नहीं है तो हमने समाज को क्या दिया ? आईआईटी दिल्ली में कुछ सालों से, मानवीय मूल्य और तकनीकी का एक पेपर पढ़ाया जा रहा है जिसका उद्देश्य, शिक्षित व्यक्ति की सामाजिक भूमिका को बढ़ाना है।
कुछ लोग तनाव दूर करने के लिए, योग, अध्यात्म के अलावा लिविंग विथ हंड्रेड थिंग्स जैसी योजना पर काम कर रहे हैं जिसमें कम से कम चीजों के साथ जीवन जीने को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे घरों में अनावश्यक वस्तुओं का होना भी तनाव और बढ़ते खर्च की निशानी है। परिजनों के साथ संवाद, हास-परिहास, देशाटन, प्रकृति से नज़दीकी और नंबर-नौकरी की जानलेवा प्रतियोगिता के बिना, एक अच्छे नागरिक बनने और सरल जीवन जीने की ललक हमें और हमारे बच्चों को एक लम्बी और खुशनुमा ज़िन्दगी दे सकती है। बढ़ती ज़रूरत और गलाकाट प्रतिस्पर्धा, तनाव और आत्महत्या के आंकड़ों को बढ़ा सकती है, जीवन में आनन्द नहीं ला सकती है।
-डॉ. संजीव राय
अन्य न्यूज़